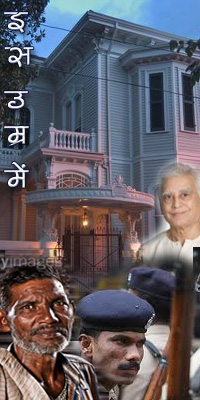 |
व्यंग्य के नाम पर, या सच
तो यह है कि किसी भी विधा के नाम पर पत्र-पत्रिकाओं के लिए
जल्दबाजी में आएँ-बायँ-शायँ लिखने का जो चलन है, उसके अंतर्गत
कुछ दिन पहले मैंने एक निबंध लिखा था। वह एक पाक्षिक पत्रिका
में ‘हास्य-व्यंग्य’ के स्तंभ के लिए था। हल्केपन के बावजूद
उसे लिखते-लिखते मैं गंभीर हो गया था (बक़ौल फ़िराक़, ‘जब पी
चुके शराब तो संजीदा हो गए’) यानी, इस निबंध से ‘शायँ’ ग़ायब
हो गई थी, सिर्फ ‘आयँ-बायँ’ बची थी।
‘आयँ-बायँ’ की प्रेरणा शहर के एक बहुत बड़े दार्शनिक ने दी थी
जो उतने ही बड़े कवि और कथाकार भी थे परंतु वास्तव में प्रेरणा
उन्होंने नहीं, उनकी मौत ने दी थी। वे एक सड़क दुर्घटना में
घायल हो गए थे। एक सप्ताह तक अस्पताल और घर की सेवा अपसेवा के
बीच झूलते हुए उनकी मृत्यु हो गई। उनके बेटे को पता था कि वे
ऊँचे दर्जे के विद्वान हैं, पर उनके प्रशंसकों और मित्रों के
नाम का उसे पता न था। इसलिए उसने एक अखबार के दफ्तर को
छोड़कर-जो उतना ही गुमनाम था-दो-चार गिने-चुने रिश्तेदारों को
ही उनके न रहने की खबर दी और वहीं आठ-दस लोग मिलकर उनका
दाह-संस्कार कर आए। बाद में उनके देहांत की खबर फैली और तब
अखबारों में विद्वानों के प्रति समाज की उपेक्षा पर जमकर लिखा
गया, यह और बात है कि उनकी मृत्यु और उसके अवसादपूर्ण कारणों
पर तब भी ज़्यादा नहीं लिखा गया। |