|
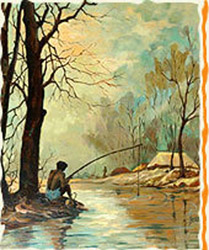 1 1
मछली
मारने का पुरुषार्थ
-पंकज परिमल
जैसे
और बहुत सारे पुरूषार्थ हैं, ऐसे ही मछली मारना भी
किसी पुरूषार्थ से कम नहीं। भले ही मछली मारने जैसे
निकृष्ट काम को इज्जत न दी जाती हो, भले ही उसे
बैठे-ठाले का काम निरूपित किया जाता हो, पर मछली मारना
सचमुच टेढ़ा काम है, मेहनत का काम है, अच्छा-खासा
पुरुषार्थ है जो ऐसे-वैसे के बस का नहीं। इस मुहावरे
के कितने रूप हैं-मछली मारना, माछी मारना। माछी के दो
अर्थ हैं- मछली और मक्खी। तो इस रूप की यात्रा करके यह
बना- ’मक्खी मारना‘ जो मछली मारने से ज्यादा टेढ़ा काम
तो है ही, शायद ज्यादा फालतू और अनावश्यक भी। मछली तो
किसी काम आती भी है पर मक्खी किसी काम नहीं आती? सिवाय
गंदगी फैलाने के और अपनी भिनभिनाहट से हमारे परिवेश
में व्यवधान पैदा करने के।
यहाँ
से मछली मारना और मक्खी मारना दो अलग-अलग किस्म के काम
बन जाते हैं। मछली मारने का तो प्रयोजन है भी, मक्खी
मारने का क्या? मारी तो मारी, नहीं मारी तो नहीं मारी।
बंदरों की तरह निरी उछल-कूद मचाने पर, जिंदगी भर की
भाग-दौड़ करने पर थोड़ी-सी अवांछनीयता परिवेश से हट भी
गई तो क्या परिवेश साफ हो जाएगा? क्या और मक्खियाँ
नहीं भिनभिनाएँगी और परिवेश को गंदा नहीं करेंगी? अतः
मक्खी मारने को, ज्यादा मेहनत के बाद शून्य बराबर
उपलब्धि के काम को भूल जाइए। यही वह बिंदु है जहाँ
मक्खी मारने के मुहावरे की भ्रांति में मछली मारने के
महत्वपूर्ण काम की इज्जत चली गई और ’झख मारना‘ जिसे
कायदे से झष या ’मछली मारना‘ समझा जाना चाहिए था, गलती
से मक्खी मारने जैसा फालतू का काम मान लिया गया और
यहीं अर्थ का अनर्थ हो गया।
मछली मारना सचमुच बड़े कलेजे का काम है। बैठे तो रहो एक
जगह वंशी पकड़े, किंतु पूरा ध्यान लगाए रखो। ज्यादा
हिलना-डुलना नहीं, पर मछली का ध्यान नहीं छोड़ना। एक
निठल्ली पर एकाग्रचित्त साधना। कौन-कौन नहीं लगा मछली
मारने में? मछुवारा लगा मछली मारने में। बगुला लगा
बक-ध्यान लगाकर मछली मारने में। और तो और,
विश्वविख्यात धनुर्धर तक लगे मछली मारने में। नहीं,
नहीं मछली मारने में नहीं, छाया मात्र तककर मछली की
आँख बींधने में चलती हुई, गोल-गोल घूमती हुई मछली की
आँख बींधने में। अर्जुन कहता- पेड़ नहीं दिखाई देता,
चिड़िया नहीं दिखाई देती, सिर्फ चिड़िया की आँख दिखाई
देती है। हमारी जिंदगी भर की साधना का निचोड़ यह है कि
हम मछली मारने में समर्थ हो सकें। कम से कम, मछली की
आँख बींधने में, उसे नजरबंद करने में दक्ष हो सकें। जो
मछली की आँख तक नहीं बींध सकेगा, वह तो स्वयंवर से भी
खाली हाथ लौटेगा। जो अपनी दक्षता को न सिद्ध कर सकेगा,
जो ’सरवाइवल ऑफ द फिटेस्ट‘ की कसौटी पर खरा न उतर
पाएगा, उसे क्या मिलेगा? न अर्थ, न काम। यो मां जयति
संग्रामे यो मे दर्पम् व्यपोहति। यो मे प्रतिबलो लोके
स मे भर्ता भविष्यति। भोग करना है तो पहले भर्त्ता बन।
भर्त्ता बनना है तो पहले मछली मारने में अपनी योग्यता
साबित कर। कमाई-धमाई करके दिखा तो मानूँ। पहले मुझे
जीत; मेरी देह को नहीं, मेरे दर्प को रौंद पहले। मैं
रूपगर्विता हूँ तो तू अर्थ की शक्ति लेकर आ, भुजबल
लेकर आ, पुरूषार्थ लेकर आ, कंचनमृग बींधने की योग्यता
लेकर आ, मछली मारने में दक्षता पाकर आ।
जितनी तरह के मछली मारने वाले हैं, उतनी ही तरह के
मछली मारने के तरीके हैं। कर्ता के बदलने से क्रिया भी
बदलती है और क्रिया का प्रयोजन भी। जिसे भर्त्ता बनना
है वह मछली के प्रति ज्यादा क्रूर नहीं होता, वह उसे
केवल बींधकर छोड़ देता है। उसे निशानेबाजी की अपनी
योग्यता साबित करनी है, भला मछली से उसकी क्या
दुश्मनी? उसकी चिंता तो मात्र इतनी है कि उससे पहले
कोई मछली मारने में सफल न हो जाए, और उसे टापते रह
जाना पड़े। वह एक तीर से दो मछलियाँ मारता है- एक तो
मछली स्वयं, दूसरे इस दक्षता के एवज में मिल सकने वाला
पारितोषिक। एक मछली मारने वाला वह है जो जल में उतरकर
खड़ा है- बक-ध्यान लगाए, कब कोई मछली पास से गुजरे, कब
वह उसे उदरस्थ करे! मछलियाँ तो अभिशप्त हैं उस लहर में
बहने के लिए जिसे वे जीवन मान बैठी हैं। इस जल में ही
उसका जीवन है और उस जल का प्रवाह ही उसका मरण। जल से
बाहर तो मरण है ही, जल के भीतर भी मरण है। भीतर इसलिए
कि जीवन अपने प्रवाह में बढ़ा जा रहा है और मृत्यु कहीं
बक-ध्यान लगाए बैठी है। वह जल के भीतर भी हमारा शिकार
कर ले जाती है। जीवन के चरम-सुख के भोग के क्षण में हम
अकस्मात छले जाते हैं। आप ठगाए सुख मिले, और ठगे दुख
होय। अगर मछली की दृष्टि से सोचें तो ठगे जाने में भी
सुख है। किसी का ग्रास बन जाने में भी सुख है। किसी की
तृप्ति का साधन बन जाने में भी सुख है। बुद्धिनाथ
मिश्र के एक प्रसिद्ध गीत का आरंभ है-
एक बार और जाल फेंक रे मछेरे
जाने किस मछली में बंधन की चाह हो !
मछेरों को ही नहीं सिद्ध करना है अपना पुरूषार्थ, जो
है तो दरअसल अर्थ और काम के पुरूषार्थ का ही एक क्रिया
रूप, अपितु मछलियों को भी सिद्ध करनी है आखेट हो सकने
में अपनी तत्परता। एक होड़-सी है मछलियों में कि जाल
में पहले कौन फँसेगी। जो आमंत्रण दे रहा है मछुवारा,
वह धीरे-धीरे हमें लुभा रहा है। जो चारा वह लटका रहा
है वह अपने मोहपाश में हमें बाँध रहा है। जो भाषा वह
बोल रहा है, उसके तर्क हमारे गले की फाँस बन गए हैं।
कहीं देर न हो जाए फँस पाने में, कहीं दूसरे के गले
में न चला जाए चारा।
मनुष्यों में, मछली मारने वाले मनुष्यों में भी दो तरह
के मनुष्य हुए- एक वो जो तट पर बंसी पकड़कर बैठता है और
दिन-भर एक-एक मछली का रास्ता तकता है। उसकी इच्छा बड़ी
सीमित है। उसकी आवश्यकता बड़ी संतुलित है। कबीर कहते
हैं-
साईं इतना दीजिए जा में कुटुम समाय।
मैं भी भूखा ना रहूँ, साधु न भूखा जाय।।
इसे कुटुम समाने की चिंता है, इसे भूखा ही सो जाने की
चिंता है। अब साधु की चिंता कौन करे, अपना भी ठिकाना
नहीं रहा! पर फिर भी यह भूखा ही सो जाता है, फिर भी
इसका कुटुम नहीं समाता। साधु तो इसके द्वार से भूखा
चला जाता है, अलबत्ता असाधु भूखा नहीं जाता। चिड़िया
भूखी उड़ जाए तो उड़ जाए, चांडाल कौआ कभी भूखा नहीं उड़ता
उसके द्वार से। परंपरा और आस्था के नाम पर या तो वह
पूज्य पितरों के नाम का अन्न कौवों को खिला दे या कौवा
बेशर्मी से उसके हाथ से झपट ले जाए- अपनी शक्ति और बल
की धौंस जमाता हुआ। ये जो अप्रत्यक्ष कर या प्रत्यक्ष
कर हम भुगतते हैं न, ये काग-ग्रास हैं जिन्हें कभी हम
अपनी श्रद्धा से देते हैं, अपना कर्त्तव्य मानकर देते
हैं तो कभी हमसे जबरन वसूल लिए जाते हैं। क्या फर्क रह
जाता है कर और हफ्ते में? अपना कुटंब समाए या न समाए,
हम भूखे सोएँ या छकें, साधु चाहे हमारे द्वार से भूखा
चला जाए, पर असाधु भूखा नहीं जाता। वह तो साधु के वेश
में आकर हमसे भिक्षा में हमारा सर्वस्व लिखवा ले जाता
है। बंसी पकड़कर बैठने वाला इसलिए भी भूखा रह जाता है
कि वह ’फिटैस्ट‘ सिद्ध नहीं हो पाता, वह योग्यतम नहीं
है, वह भलामानुष तो अवश्य है पर एक हद तक निठल्ला है।
वह मछली के आकर फँसने की दिन-भर प्रतीक्षा करता है और
अक्सर छूँछे हाथ उठ जाता है। उसके छूँछे रह जाने के
पीछे एक कारण और भी है। वह स्वयं को मछली से इतर जीव
मानता है। वह मछलियों में मछली बनकर रह पाना जानता तो
बड़ी मछली द्वारा छोटी को उदरस्थ करने की कला से भी
परिचित हो पाता। वह बड़ी मछली नहीं बन पाया तो छोटी
मछली उसे मिली ही नहीं हैं। पर इस बेचारे का भी फंदा
कभी-कभी खाली रह जाता है। क्योंकि यह युक्ति तो साधना
है, श्रम नहीं करता। युक्ति कभी काम आ जाती है, कभी
नहीं। कर्म या श्रम भी कभी फल प्राप्त कर लेते है तो
कभी यह ’मा फलेषु कदाचन्‘ कहकर मन को बहलाने का कारण
बन जाता है।
सबसे घाघ, सबसे चतुर, सबसे श्रमशील है वो मछुवारा, जो
समुद्र में कूद पड़ा है, ढेर सारे प्रलोभन लेकर,
लंबा-चौड़ा जाल लेकर, मछलियाँ घेर सकने की लंबी-चौड़ी
महत्वाकांक्षी योजना लेकर। परवाह नहीं उसे समुद्र की
सर्वग्रासी लहरों की, वह कमर तक कूद पड़ा है समुद्र
में-अकेले नहीं, पूरे दल-बल के साथ। युक्ति के नाम पर
लहरों के अनुमान पढ़ता हुआ, समुद्र का मूड भाँपता हुआ,
पूरी सोची-समझी रणनीति के साथ समुद्र में उतरता है
मछुवारा। एकाध नहीं, राशि की राशि मछलियों की चाह है
उसे। वह पूरी तैयारी से लैस है। मछलियों के मूड और
प्रवृत्तियों पर उसके शोध, मौसम और समुद्र के बारे में
उसके पूर्वानुमान, इसके साथ ही मछलियों में से किसी एक
को अपना प्रवक्ता बना डालना- कुछ भी तरीका आजमाने से
वह नहीं छोड़ता। मोल नहीं तो ऋण, ऋण नहीं तो उधार, उधार
नहीं तो मुफ्त, अब तो आओ मछलियों ! वह मछलियों के बीच
मछली बनकर घुस जाता है और मछलियों की भाषा बोलने लगता
है, फिर धीरे-धीरे मछलियों को अपनी भाषा सिखाने लगता
है। अब इस दौर में चारे की छोटी-मोटी गोली लटकाने से
काम न चलेगा, ठोस माल फेंकना पड़ेगा समुद्र में, ऐसा
माल कि मछली नहीं, मछलियों के झुंड दौड़े चले आएँ। अब
समुद्र में गहरे में पैठकर रत्न तो मिलने से रहे, सो
मछलियाँ ही क्यों न मारी जाएँ!
जब भी घातक बनती है निसर्ग के पार जाने की चाह घातक
बनती है। जब भी शिकार करती है तो महत्वाकांक्षा शिकार
करती है। अपने परिवेश से मोह न कर पाने का मोल चुकाना
पड़ता है हमें। हम समुद्र में पले-बढ़े तो निश्चित ही
हमारी दोस्ती होगी शंख और सीपियों से, निश्चित ही
प्रवाल की रंगीन और कलात्मक शाखाएँ हमारे सौंदर्य और
हमारी अभीप्सा का चरम होना चाहिए था, लेकिन हमारे इस
नैसर्गिक जीवन के बीच, हमारे इस परिवेश में किसी दूसरे
ग्रह-उपग्रह से टपके हुए अजनबी की तरह यह नई
महत्वाकांक्षा कहाँ से चली आई? चारे के रूप में यह
खाद्य कहाँ से चला आया जिससे हमारा परिचय ही न था?
बाजरे की, और तो और गेहूँ की हमारे नथुनों में तृप्ति
की गंध भरने वाली रोटी की जगह नई भूख का नया प्रतिमान
बना हुआ-सा यह पिज्जा कहाँ से चला आया? या इस जैसे
कितने ही और-और अपरिचित-से, हमारी भूख को आवाज देते,
हमारे तृषित अधरों पर चाहतों की जीभ फेरने को मजबूर
करने वाले नए-नए उपादान चले आए? जो इन्हें दिखाता गया,
मछलियाँ उसी की हो लीं, उन्होंने उसी की शर्तें
स्वीकार कर लीं, उन्होंने उसे ही अपना भाग्यविधाता मान
लिया। शंख-सीपी और प्रवालों से भरे परिवेश से बाहर जो
झाँकने की कोशिश की तो हम कहीं के न रहे।
धनुर्धर, धनुर्विधा-विशारद के लिए मछली एक उत्तम
लक्ष्य है। लक्ष्य है अपनी दक्षता सिद्ध करने का। वह
भी कौन-सी मछली? चक्राकार घूमती मछली। जल की सतह छोड़कर
आकाशकुसुम की तरह आकाश में दोलायमान मछली। जैसे
आकाशकुसुम नहीं होता, ऐसे ही आकाश में मछलियाँ भी नहीं
होतीं। फिर भी फिर भी लगता है कि आकाश में मछली है।
द्रौपदी-स्वयंवर का केंद्र बनती हुई मछली। कोई इसे
बींध पाए तो मजा आ जाए। पर होता यह है कि मछली को बींध
तो पाता है कोई एक, पर अपने-अपने तर्क को लेकर
हिस्सेदार बन जाते हैं कई। काम और पुरूषार्थ एक का, पर
मिल-बाँटकर खाएँ सब- पाँच पांडवों की तरह। भोक्ता बनने
को सब तैयार पर भर्त्ता बनने को कोई तैयार नहीं।
अद्भुत है यह सामाजिक न्याय! अद्भुत है फल की यह
बंदर-बांट! पर जो भोक्ता बनेगा, उसे भी फल के हित के
लिए कुछ न कुछ यत्न तो अवश्य करना पड़ेगा, पर जिसे
प्राप्त करने में मेहनत नहीं पड़ी, उसका मोल उसे पता भी
क्या? उसे दाँव पर लगाने में झिझक कैसी? जो हमें सहसा
उपलब्ध हो जाए उसके प्रति कैसा भी सलूक करें, किसी को
भी दे डालें, क्या यह उचित है? एक कहावत सुनी थी-
सुगड़ भलाई ससुरा लेय
भैंस खोल बहू की देय।
बहू मायके से दहेज में लाई थी भैंस तो ससुर जी दानी बन
गए। अब बरजेगी बहू तो बहू बुरी हो गई। पर फल की रक्षा
के लिए किसी को तो बुरा होना पड़ेगा- कभी न कभी, किसी न
किसी क्षण। भीम अपने दाँत किटकिटाकर रह जाता है।
’बलमसि बलमहि देहि‘ से काम नहीं चलेगा, ’मन्युरसि
मन्युमहि देहि‘ भी चाहिए। हम कभी न कभी जंघा तोड़ने का
संकल्प उठाएँगे तो जंघा टूटेगी जरूर। जरूरी है कि यह
प्रतिरोध कर सकने की ऊर्जा बची रहे, उससे ज्यादा जरूरी
है कि प्रतिरोध करने का संकल्प बचा रहे। धनुर्धर के
लिए, बुद्धि और बल के धनी के लिए मछली के प्रति एक
लक्ष्य-भाव है, लक्ष्य-साधक का भाव। यह क्रूर नहीं है।
इसलिए क्रूर नहीं है क्योंकि मछली से उसकी जाती
दुश्मनी नहीं है। वह मछली का दृष्टिबंधन करता है, वह
उसे नजरबंद करता है। नजरबंद मछली अपने आखेटक को नहीं
देख पाती। वह मग्न है। उत्कर्ष के आसमान में गोल-गोल
घूमने में मग्न है। नजरों पर पट्टी बँधे हुए
दृष्टिबंधित कोल्हू के बैल की तरह मग्न है, जो घूम रहा
है और गले में बँधी हूई घंटियों की रूनक-झुनक
सुन-सुनकर आनंदमग्न हो रहा है और उससे जो तेल निकल रहा
है, उससे तो किसी और का ही पात्र भर रहा है। आखिर में
थोड़ी खली-भर मिल जाए तो पर्याप्त। इन सब कारणों से
मरना नहीं, पर दृष्टिबंधन का होना बहुत जरूरी है।
द्ष्टि-विदग्ध नायिका कहती है-
कागा सब तन खाइयो, चुनि-चुनि खइयो माँस।
दो नयना मत खाइयो, पिया दरस की आस।।
पर जो कागा है, बहुत सयाना है। उसने तन तो छोड़ दिया
क्योंकि तन से तो अभी बहुत काम लेना है। बहुत पेरना है
उसे कोल्हू में और अपना उल्लू सिद्ध करना है। वह सारा
शरीर छोड़ देता है, बल्कि उसे पालता-पोसता है जतन से,
किंतु पहले आँखें खाता है। आँखें न रहेंगी तो हम काग
के विरूद्ध अपनी साक्षी न दे सकेंगे। अपने विरूद्ध रची
जाती हुई दुरभिसंधियों को न जान सकेंगे।
शिकारी, नहीं-नहीं मछुवारा भी मछली को मारता नहीं है।
उसके पास कई विद्याएँ हैं। वह सभी को आजमाता है- मारणं
मोहनं वश्यं स्तंभनोच्चाटनादिकम्। वह कभी मारण करता है
तो कभी मूर्च्छन करके छोड़ देता है। मोहन-मूर्च्छन
करेगा तो जीवन-भर अपना अभीसिप्त सिद्ध करता रहेगा।
इतनी साँस तो चलती रहे जो हम व्यापारी से कर्ज लिए भोग
की किस्तें भरते रहें। अब हम इस मूर्च्छा में से ही
प्रगाढ़ निद्रा की ओर सरक लें तो किसी का क्या दोष? पर
इस हालत में भी दाता का नुकसान नहीं है। आम के आम तो
गुठलियों के दाम। हमारे चाम का मोल लगे न लगे, हमारी
लाश को मोल जरूर लग जाएगा। बीमा कंपनी जो बैठी है
महाजन की हितू बनकर। वह हमारा दोहन करता है। दोहन करता
है कि उसके हमारे प्रति किए जाते हुए अपकार और अपराध
हमें दृष्टिगत नहीं होते, या उसके कृत्य में हमें अपना
उपकार होता मालूम देता है। जैसे गोपियाँ भूल जाती हैं
यमुना-तट से कन्हैया द्वारा चीरहरण और वह चीरहरण न
रहकर चीरहरण-लीला बन जाता है, ऐसे ही व्यापारी द्वारा
आयोजित सौंदर्य प्रतियोगिताओं में ललनाएँ दिगंबरता को
प्राप्त करके स्वयं को दिव्याभरण भूषिता समझने लगती
हैं। वह उसकी सौंदर्य दृष्टि का अपनी देहयष्टि पर
अनुग्रह तक मानने लगती हैं, अभिभूत हो जाती हैं
प्रशंसा के दो बोल और रूप की विशद ख्याति पाकर। वह
हमारा वशीकरण करता है। हमसे वह चाहे जो काम ले ले। हम
उसकी स्वामिभक्ति में चाहे जो कर डालें। खुद को मारना
हो या दूसरों को खुद फँसना हो उसके जाल में या दूसरों
को फाँसकर लाना हो, अपना आहार जुटाने के भ्रम में बँधे
हम दूसरों का आहार जुटाने का साधन बन जाते हैं।
वह हमारा स्तंभन कर डालता है। स्तंभित हो जाते हैं हम।
टस से मस नहीं हो पाते। अचानक हम पर अनुग्रह की वर्षा
हुई और हम स्तंभित हो गए। अप्रत्याशित रूप से किसी बड़ी
कंपनी के मानव संसाधन प्रबंधक की नजर गुरूकुल में ही
हम पर पड़ गई तो हम उसके द्वारा बिछाए जाल में स्तंभित
हो रहे। मूर्च्छित नहीं हुए, वशीभूत हो गए।
वह हमारा उच्चाटन करता है। हमारे चित्त में विभ्रम
पैदा कर देता है। दुविधा कहीं का नहीं रहने देती, न घर
का, न घाट का। हम तय नहीं कर पाते कि किस ओर जाएँ।
धारा के खिलाफ जाएँ या धारा के अनुगामी बनकर उसके जाल
के फैलाव को अपनी नियति स्वीकार कर लें? वह हमारा
विवेक भले ही न मार पाया हो, पर उच्चाटन फैलाने में वह
जरूर कामयाब हो गया है। धारा के खिलाफ जाने का साहस
सबमें नहीं होता। हमारा जो बचा-खुचा विवेक है, वह धारा
की अनुकूलता में ही हमारा पथ दिखाता है। दिखाता है कि
हमारी मुक्ति जाल से नहीं है। बस, तय तो हमें अब इतना
करना है कि इस जाल में फँसें या दूसरे। इतना सयानापन
तो हममें अब तक आ ही जाना चाहिए कि जालों के परस्पर
गुण-दोष की और शिकारी-शिकारी की नीयत में या उसके
प्रलोभनों के पैकेज में से विवेचन करके अपने लिए किसी
उपयुक्त एक को विकल्प के तौर पर चुन सकें क्योंकि
मछलियों में ही नहीं है प्रतियोगिता फँसने की,
शिकारियों के मध्य भी है। इस समय में यह दोनों के लिए
मुश्किल-भरा दौर है- जितना मछली के लिए, उतना ही
शिकारी के लिए। यह दोनों के लिए ही योग्यतम की
उत्तरजीविता वाली कसौटी है जिस पर खुद को साबित करना
है अन्यथा छोटी मछली को बड़ी मछली का ग्रास बनते देर
नहीं लगेगी।
२२ जुलाई २०१३ |