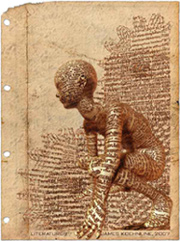
प्रवासी हिंदी साहित्य में
परंपरा, जड़ें और देशभक्ति
- मनोज
श्रीवास्तव
क्या
प्रवासी हिन्दी साहित्य पछतावे का साहित्य होकर ही
जड़ों का या देशप्रेम का साहित्य हो सकता है? कि
जिसके चरित्र पीछे मुड़कर देखने की प्रक्रिया में लीन
हैं? कि उस साहित्य में बार-बार ऐसे चरित्र आते हैं
जो अलग अलग परिस्थितियों से एक ही जगह पहुँचते हैं
जहाँ वे अपने अभी तक जिये हुए का पुनर्निरीक्षण कर रहे
होते हैं? अपने जीवन के अभी तक चले आए संस्करण की
किसी न किसी बहाने से समीक्षा। इस समीक्षा में कहीं
साहस होता है तो कहीं संकोच। लेकिन अधिकतर यह बहुत
घटना-बहुल साहित्य नहीं है, यह मनोवैज्ञानिक
प्रतिक्रियाओं का साहित्य है। कहीं पाले हुए भरम टूटते
हैं तो कहीं कुछ नए भरम बनते हैं। कही निराशा है तो
कहीं घिन। भीतर ही भीतर इन कहानियों और कविताओं में एक
प्रतिरोध सा
पकता रहता है।
प्रवासी होना एक लगातार कायाँतरण में रहना है। खासकर
तब जब साहित्यकार होने के नाते आपके संवेदन-तंतु कुछ
ज्यादा ही जागृत हों। यह देखकर आश्चर्य होता है कि जिन लोगों को
हिन्दुस्तान का आम आदमी समृद्ध मानता है, उनका साहित्य
स्वयं में स्थैर्य का साहित्य कतई नहीं है।
प्रवासी हिन्दी लेखकों की त्रासदी यह नहीं है कि वे विदेशी
धरती पर पैर रखकर लिख रहे हैं, त्रासदी यह है कि जब इतने बरसों
बाद वे भारत भूमि पर पैर रखते हैं तो वहाँ कुछ विदेशी-सा हो
गया है, वहाँ कुछ पराया-सा हो गया है। प्रवासी हिंदी लेखक एक
तरह की दोहरी जिम्मेदारी में, रहता
है। वह कहीं भी यात्री नहीं है। यात्रा उसमें दिखेगी भी तो
वैसे जैसे उषाराजे सक्सेना के कथा संग्रह ‘प्रवास में’ की
तरह-या इसी संग्रह की कहानी ‘यात्रा में’ की तरह। यात्री होना
तो दायित्व-मुक्ति है। प्रवासी होना दायित्व का दुगुना होना
है। यात्री को सुविधा है कि वह ‘अज्ञात भूमि’ के बारे में,
लिख सकता है। प्रवासी की मुश्किल
है कि वह यात्री नहीं है, वासी है, हालाँकि एक खास तरीके का
वासी है जिसके चलते ‘प्र’ उपसर्ग अपने तरह से सार्थक होता है।
इसलिए प्रवासी लेखक की दृष्टि पर्यटक-निगाह नहीं है। यात्री की
तरह प्रवासी भी सरहदें पार करता है, लेकिन उसके साथ साथ वह
अपने आवरण भी तैयार करता चलता है।
मैंने यात्री-साहित्य
भी पढ़ा है और प्रवासी-साहित्य भी। लेकिन कम से कम हिन्दी की
इन दोनों धाराओं को देखूँ तो मुझे लगता है कि प्रवासी-साहित्य
में कहीं भी उतना आत्म-आश्वस्ति का भाव नहीं है जो
यात्री-साहित्य में है। प्रवासी साहित्य का अंतर्द्वन्द्व जड़
से उखड़कर जमने का अंतर्द्वन्द्व है। मुझे यह भी लगता है कि
आत्म-आश्वस्ति की इस कमी के
कारण प्रवासी-साहित्य में ज्यादा
मार्मिकता आ पाई है, वह ज्यादा अन्तःस्पर्शी बन पाया है।
मुझे ज्ञात हुआ कि हंस के सम्पादक राजेन्द्र यादव जी ने जामिया
मिलिया विश्वविद्यालय के एक कार्यक्रम में कह दिया कि
तेजेन्द्र भाई को शायद बुरा लगे, अभी जो प्रवासी साहित्य के
नाम पर परोसा जा रहा है, उसका स्तर कुछ खास नहीं है। भारत में
रचे जा रहे साहित्य के सामने प्रवासी साहित्य का कोई कद उभर कर
नहीं आता।’’ मैं नहीं जानता कि राजेन्द्र यादव जी ने यह
इम्प्रेशन कैसे संचित किया। मैं तेजेन्द्र जी द्वारा दी गई उस
प्रतिक्रिया से भी बहुत सहमत नहीं हूं कि ‘‘मैं प्रवासी
साहित्य जैसे आरक्षण कोटे को मानता ही नहीं। मुझे तमाम आरक्षित
साहित्य से एलर्जी है। मैं साहित्य को महिला लेखन, दलित लेखन,
सवर्ण लेखन, प्रगतिवादी लेखन आदि आदि में बाँटने के सख्त खिलाफ
हूं। अब एक नया आरक्षण-प्रवासी साहित्य। क्या है यह प्रवासी
साहित्य।’’ मैं राजेन्द्र-तेजेन्द्र दोनों के तर्कों से
आश्वस्त नहीं हो पाता। तेजेन्द्र जी जब इस तरह के वर्गों का
विरोध करते हैं तो वे शायद संवेदना के उन विशिष्ट कोणों में
निहित सृजनात्मकता की संभावनाओं को वैसे ही एप्रीशिएट नहीं कर
पाते, जैसे राजेंद्र जी प्रवासी लेखन की उपलब्धियों को नहीं कर
पाते। यही विनम्र असहमति मेरी डॉ. प्रभाकर श्रोत्रिय के उस कथन
से है जो उन्होंने साहित्य अकादमी के सभागार में अमेरिका के
हिंदी कथाकारों के संग्रह ‘कथांतर’ को लोकार्पित करते हुए कहे
कि एक अच्छी रचना मुख्यतः मनुष्यता के किसी आयाम की अभिव्यक्ति
होती है। उसे वर्गों/खानों/विमर्शों में बाँटना उचित नहीं।
हिन्दी का कुछ सर्वश्रेष्ठ जो है वह प्रवासी परिस्थितियों में
ही लिखा गया। क्या राजेंद्र जी को निर्मल वर्मा की चीड़ों पर
चाँदनी, हर बारिश में, धुँध से उठी धुन और वे दिन कृतियों की
याद है? उन्हें लिखते वक्त निर्मल वर्मा प्राग में प्रवासी थे।
निर्मल दस साल प्राग में रहे थे। नयी कहानी राजेंद्र यादव की
जितनी ऋणी है, उससे कम ऋणी निर्मल वर्मा की नहीं है। निर्मल
वर्मा की परिन्दे, जलती साड़ी, लंदन की रात, पिछली गर्मियों
में उनके प्रवासी भारतीय होने के वक्त की रचनाएँ हैं।
संवेदनाओं की जितनी बारीक पर्त पर निर्मल जी ने काम किया, वह
हिंदी को प्रवासी संवेद्यता की एक अद्भुत देन है। यदि
फणीश्वरनाथ रेणु हिन्दुस्तान की जमी रमी हुई जड़ों के महान
कृतिकार थे तो निर्मल वर्मा जड़ों से उखड़ जाने के उतने ही
महान रचनाकार। प्रवासी परिपेक्ष्य का हिंदी साहित्य में महत्व
कम करके राजेंद्र यादव यदि अपने स्मृति-भ्रंश का परिचय देते
हैं तो उस पर्सपेक्टिव को एक सामान्यीकरण में गुम करके
तेजेन्द्र भी न्याय नहीं कर रहे। आखिरकार जड़ का जीवन में
जितना महत्व है, उससे कम महत्व सेतु का नहीं है। यह आश्चर्य
नहीं कि प्रवासी रचनाओं के अनिल जोशी कृत एक संग्रह का नाम
‘‘धरती एक पुल’’ ही है।
प्रवासी साहित्य ने हिंदी में
मनोवैज्ञानिक और सांस्कृतिक द्वंद्व का जो अनुभव दिया है, एक ही
समय घर से दूर होने का दर्द और घर से दूर होने की जरूरत का-वह हमारी भाषा की एक बड़ी रचनात्मक
पूँजी हैं। तेजेन्द्र शर्मा की कहानी ‘पासपोर्ट का रंग’’ के दो
रंग इसी दोहरेपन के प्रतिनिधि हैं। फणीश्वरनाथ रेणु ‘आवास’ के
रचनाकार थे, निर्मल वर्मा ‘प्रवास’ के। मुझे आश्चर्य है कि
कमल किशोर गोयनका ‘‘हिन्दी का प्रवासी साहित्य’ इस शीर्षक से
लिखे अपने बहुत लम्बे निबंध में निर्मल वर्मा का कोई जिक्र तक
नहीं करते। हाँ, यह अवश्य है कि निर्मल वर्मा यूलीसस की तरह थे
जो दुनिया भर में प्रवास कर लेने के बाद घर लौट आए थे। लेकिन
गोयनका जी पं. तोताराम का तो उल्लेख करते हैं जो फिजी में
इक्कीस
वर्ष रहकर लौट आए थे। आज के बहुत से प्रवासी हिंदी साहित्यकार
रिनैसां युग के आदर्श पैट्रार्क की तरह हैं जो कभी घर नहीं
लौटा। निर्वासित ही रहा।
निर्मल का दस साल का चेक-प्रवास जिन
आँखों से उन्होंने देखा; कभी-कभी मेरा मन होता है, उन्हीं
आँखों से भगवान राम का चौदह साल का प्रवास कहीं देखा जा सकता। वह
भी एक निर्वासन था। हमारी संस्कृति के ताने बाने रचने वाले
दोनों ग्रंथ- रामायण और महाभारत दोनों ही, निर्वासन
को कथानक बनाकर चलते हैं। दोनों ही निर्वासन के घाव से उसी तरह
रक्तरंजित हैं जैसे हमारे बहुत से प्रवासी साहित्यकार। और यह
भी देखिए कि गोयनका जी के इतने भारी भरकम लेख में कृष्ण बलदेव
वैद जैसा विद्रोही प्रवासी साहित्यकार भी सिरे से गायब है। वे
ब्रांडीज़ विश्वविद्यालय और स्टेट यूनिवर्सिटी आफ न्यूयार्क
में इतने सालों से पढ़ा रहे थे। चालीस के करीब किताबें लिख चुके
थे -उपन्यास, कहानियाँ, नाटक, निबंध, डायरियॉ। एक नौकरानी की
डायरी, हमारी बुढ़िया, मायालोक, काल कोलाज़, लापता, वह और मैं,
उसके बयान, बदचलन बीबियों का द्वीप, भूख आग है, बीच का दरवाजा,
गुजरा हुआ जमाना, मोनालिसा की मुस्कान, शिकस्त की आवाज जैसी
अद्भुत कृतियों से भरपूर उनका पचास साल का बहुत मौलिक, बहुत
विद्रोही और बहुत नयापन भरता हुआ साहित्य रिश्तों की निर्दयता,
हिंसा, पिशुनता और टुच्चेपन को इतनी बारीकी से चीन्हता है।
विजय चौहान जिन्होंने धर्मक्षेत्रे कुरूक्षेत्रे, एक बुतशिक़न
का जन्म, अफसर की बेटी, जैसी अद्भुत कहानियाँ दीं -उन्हें
हिन्दी में किस तरह से
कमतर माना जा सकता है?
प्रवासी होने से अनुभूतियों की उद्दामता और गांभीर्य में कोई
गिरावट नहीं होती। भाषिक तैयारी पर भी कोई असर नहीं पड़ता।
क्या टॉमस मॉन स्वयं १९३३ के बाद से १९५५ तक स्वयं एक प्रवासी
साहित्यकार नहीं था? क्या बर्तोल्त ब्रेख्त, हेनरिक मान,
हर्मेन ब्रोच, एमिल लुडविग, ब्रूनो फ्रैंक का साहित्य उनके
प्रवासी मानस का प्रतिबिंब नहीं है और क्या ऐसा होने से उसका
साहित्यिक मूल्य वैसे कमतर हो गया जैसे राजेन्द्र यादव कहते
हैं? क्या अब्राहम काहन का प्रसिद्ध उपन्यास ‘द राइज आफ डेविड
लेविंस्की’ एक प्रवासी की ही कथा नहीं है। और क्या वहाँ भी
नायक भौतिक रूप से अत्यन्त सफल होकर भी यह नहीं महसूस करता कि
उसकी सफलता की कीमत उसकी आत्मा का परिणाम है-वह आत्मा जो घर
की लोक-पंरपराओं में उससे कहीं ज्यादा जड़ें जमा चुकी थी जितना
वह सोचता था।
मिशेल गोल्ड का ज्यूस विदाउट मनी, लोर सेगल का
‘हर फर्स्ट अमेरिकम, आई.बी.सिंगर का ‘शैडोज ऑन द हडसन’, मारियो
पूजो का ‘द फार्चुनेट पिल्ग्रिम’, ओ.ई. रोल्वाग का ‘जाइंट्स इन
द अर्थ’, विला कैथर की ‘माई एँटोनिया’ जैसे उपन्यास प्रवासी
अनुभव के मास्टर पीस रहे हैं। इनमें रचनाकारों को अपनी भाषा के
देशज प्रांतर से निकलकर एक आंग्ल माहौल में जाना पड़ा किंतु
उससे रचना की गुणवत्ता दुष्प्रभावित नहीं हुई। इसलिए यदि आज
कुछ प्रवासी रचनाएँ भर्ती की लगती हैं तो यह भी समझना होगा कि
वे उसी प्रकार प्रवासी साहित्य की प्रतिनिधि नहीं है जैसे
गुलशन नंदा देशी हिंदी साहित्य के प्रतिनिधि नहीं थे।
जर्मनी में एक शब्द था इलेंड जिसका मूलार्थ थाः विदेशी भूमि।
बाद में उसका अर्थ बिगड़ते बिगड़ते तकलीफ हो गया।
बहुत-सा प्रवासी साहित्य इसी तकलीफ का साहित्य है। यह तकलीफ
जरूरी नहीं कि जिस देश में प्रवासी रहता है, उसके प्रति आभार
का अहसास न करने वाली तकलीफ हो। यह तकलीफ वैसी भी हो सकती है
जैसी कनाडा के प्रवासी हिंदी लेखक सुमनकुमार घई की कहानी ‘लाश’
में है जहाँ प्रवासी मां बाप अपने बच्चों पर ऐसी बंदिशें लगा
देते हैं जो कि स्वयं उन्होंने स्वदेश में नहीं झेली थीं। घर
प्रवासी रचना में एक तरह की परिचितता और सुरक्षा, एक तरह के
शरण्य और स्मृति, एक परंपरा और सुविधा, एक लोकस और एक धुरी की
तरह आता है। जैसा कि अबूधाबी के प्रवासी लेखक कृष्णबिहारी अपनी
कहानी ‘इंतजार’ में कहते हैं- ‘तब दुनिया कितनी मीठी हुआ करती
थी।’ या कल्पना सिंह चिटनिस अपनी कविता में लिखती हैं- उनकी
स्मृतियों में हैं……./उनका घर/और घर के पिछवाड़े खिला अकेला
फूल/उनकी स्मृतियों में है और/उनके संवाद, कहकहे और मीठीधूप या
मार्तिन हरिदन्त लछमन कहते हैं- कई देशों के मौसम का/स्वाद
लेकर/पूरी पृथ्वी के
ऊपर/मेरी यात्रा की वापसी होती है। एक चिड़िया की तरह/वृक्ष की
टहनी पर/संध्या बेला में।
प्रवासी साहित्य की अधिकतर रचनाएँ कभी वर्तमान और कभी विगत के
बीच इतनी जल्दी जल्दी शिफ्ट करती हैं कि वे कई बार कहानी से
ज्यादा कहानीकार की अंतर्कथा बताती चलती हैं। एक ऐसे रचनाकार
की जो रहता कहीं है और जिसे याद कहीं और का यथार्थ आता रहता
है। जैसे उसके दिल के भीतर एक पाठ के अंदर एक दूसरा
पाठ बन रहा है। कभी कभी भीतर का या कहें कि केन्द्रीय
पाठ बाहर के या परिधि के पाठ को काटता है। थोड़ा उथला
हुआ तो फहीम अख्तर की कहानी ‘कुत्ते की मौत’ की तरह, गहरा हुआ
तो दिव्या माथुर की ‘फिक्र’ जैसा। दरअसल दिव्या जी की रचनाओं
में मैंने शुद्ध पाश्चात्य का निरादर कहीं नहीं देखा। वहाँ
‘खल’ वह है जो अपनी स्मृति और संस्कार से अपभ्रष्ट हो गया है।
जैसे उषा राजे सक्सेना की कहानी ‘एलोरा’ का भारतीय पिता।
विदेशी चरित्र इनमें जबरन ही खलनायक नहीं बना दिए जाते। मसलन
उषा राजे की ही डैडी कहानी का फैंरक। वह अपने प्रति पाठक के मन
में सम्मान जगाता है। यही परिपक्वता शैल अग्रवाल की कहानी
‘दीये की लौ’ में दिखाई पड़ती है, या उषा राजे सक्सेना की
कहानी ‘वाकिंग पार्टनर’ में। उषा वर्मा की कहानी ‘कारावास’ की
सैली भी एक ऐसा ही चरित्र है जिसके प्रति कृतज्ञ हुआ जा सकता
है। सांस्कृतिक अपभ्रष्टों की बात दूसरी है। उनके लिए दिव्या
माथुर की रचनाओं में एक उचित कड़वाहट भी है, जैसे ‘बचाव’ कहानी
में।
इसका मतलब यह नहीं कि प्रवासी रचनाकार कड़वाहट और
कृतज्ञता के बीच ही घूमता है। दिव्या माथुर को ही देखें। वे
मजे लेने के लिए भी कहानी लिख मारती हैं, जैसे ‘सौ सुनार की’
जिसमें मुहावरों-कहावतों का जैसे एक बम्बार्डमेंट है, जैसे एक
अप्राप्य स्वदेश को किसी और तरीके से नहीं तो ऐेसे ही पा
लिया जाए। मुहावरों-कहावतों को दुहराकर खोए हुए लोक को
खोज निकालने की कोशिश की जा रही है। कुछ तो है जो बाकी सारी
चीजों, साजो सामान, लकदक और विनोद के बीच अप्राप्य हो गया है।
उनकी ‘उत्तरजीविता’ नामक कहानी एक मरी हुई चुहिया पर है जिसे
पढ़कर मुझे अज्ञेय की ‘धैर्य-धन गदहे’ पर लिखी कविता याद हो
आई। प्रयोगवादी सौंदर्यबोध की दृष्टि से जैसे वह कविता एक
स्थान रखती है, उसी तरह से प्रवासी के मन में किसी कहावत की
तरह शेष रह गए लोक-विश्वास पर लिखी इस कहानी का भी एक
अपना ही वजूद है।
प्रवासी साहित्य हमेशा ही प्रवास से मोह-बाधाग्रस्त साहित्य नहीं है। कई बार प्रवासी परिवेश वहाँ संदर्भ तक के लिए
भी उपलब्ध नहीं है। उदाहरण के लिए उषा प्रियंवदा की ‘वापसी’ या
सौमित्र सक्सेना की ‘लड़ैती’ जैसी कहानियाँ भारत के किसी भी
हिस्से की कहानियाँ हो सकती हैं। भारत इन रचनाओं में कई बार
बिना किसी तुलनात्मक तर्क के, एकदम स्वायत्त रूप से भी मौजूद
है। भारत की स्मृति या पुनर्रचना प्रवासी साहित्यकार के मन को
एक तरह के नैरंतर्य का आश्वासन उस वक्त देती है, जब उसके भीतर
कुछ टूट गया है। ये उसके भीतर तब यौगिकता या ‘बांडिंग’ पैदा
करती हैं जब वह कुछ तोड़ आया है। यह तोड़ आने के बाद बहुत लंबा
वक्त गुजरने का इंतजार भी नहीं है। क्योंकि यह एक मनोवैज्ञानिक
समय है। पूर्णिमा वर्मन की कहानी ‘जड़ों से उखड़े’ में भारत से
आए हुए कुछ घंटे ही हुए हैं। इसलिए नास्टल्जिया इन रचनाओें में
एक तरह की सांस्कृतिक वस्तु (कल्चरल कमोडिटी) बनकर आता है।
वैसे भी नास्टल्जिया का व्युत्पत्तिगत अर्थ ‘यर्निंग फॉर
यस्टर्डे’ नहीं है, बल्कि घर वापसी की लालसा है।
नास्टल्जिया
शब्द जिन दो शब्दों से मिलकर बना है उसमें दवेजवे का अर्थ है
घर वापसी और नास्टोस का अर्थ है तृष्णा। अतः यह शब्द समय से
उतना सम्बद्ध नहीं है, जितना स्थान से। शायद इसीलिए प्रवासी
साहित्य में भारत हमेशा एक ऐसे स्थान की तरह रहता है जो जितना
प्राप्त था, उतना प्राप्य है। प्रवासी मानस अतीतजीवी नहीं है,
भारतजीवी है। अतीत तक लौटना असंभव है, लेकिन भारत लौटना हमेशा
मुमकिन है। इसीलिए सुधा ओम ढींगरा अपने गीत में कहती हैं-
साजन/मोरे नैना भर भर आवे हैं/देस की याद में छलक छलक जावे
हैं। कृष्ण बिहारी की कहानी इंतजार में भी एक वापसी है। यह बात
जरूर है कि भारत स्वयं प्रवासी के लिए एक भिन्न समय है। समय
उसके बचपन का। समय उसके पुरखों का। भारत उसके लिए किसी स्थान
तक पहुँचना नहीं है। वह उसके लिए एक टाइम मशीन में बैठना भी है
और काल के प्रति लेखक की सम्पूर्ण असहायता के खिलाफ एक विद्रोह
भी है।
समय के खिलाफ ऐसा ही एक प्रतिकार दिव्याजी
२०५० नामक
कहानी में करती हैं। भारत समय और स्थान को अन्तः परिवर्तनीय
बना देता है। भारत लेखक को कोई भावुकता में
भर देने वाला संदर्भ नहीं है। भारत उसे एक ऐसी सामर्थ्य देता
लगता है जिससे ‘बियान्ड रिकॉल’ माने जा रहे समय के सामने
प्रवासी संवेदना एक आत्मविश्वास के साथ खड़ी हो सकती है। कई
बार यह सामर्थ्य भारत के सद्गुणों पर ही उद्भूत नहीं होती,
भारत की खराबियों से भी पैदा होती है। दिव्या माथुर की बहुत ही
प्यारी कहानी ‘अंतिम तीन दिन’ पढ़िए। उसमें भारत के एक शहर
पटना की गुंडागर्दी से टकराने की इच्छा मरने का इंतज़ार कर रही
स्त्री के रोम रोम को इतना स्पन्दित कर देती है कि उसे लगता है
कि इतनी ज़िन्दा तो वह जीवन में पहले कभी नहीं रही। इसलिए इस
नास्टाल्जिआ को तृष्णा से कहीं ज्यादा सम्बद्वता के रूप में देखना चाहिए। भारत इस कारण किसी
देशभक्ति के राजनीतिक अर्थ में नहीं, बल्कि उपर्युक्त
मनोवैज्ञानिक अर्थ में प्रवासी लेखक की रचनाओं में घटित होता
है। भारत की भिन्नता का यह अहसास लेखक की पृष्ठभूमि से नहीं
होता, उस मंच से होता है जिस पर वह खड़ा है।
प्रवासी साहित्यकार के हृदय में भारत के साथ कोई अमर रोमांस चल
रहा हो, यह जरूरी नहीं। वह अपने बर्ताव में भारत के साथ काफी
तटस्थ भी हो सकता है। फिर भी भारत एक अनिवार्य क्षितिज है।
जहाँ से सिर्फ कुछ गुजरी हुई छायाएँ ही प्रवासी लेखन में नहीं
फैली है, बल्कि कुछ आलोक भी फूट पड़ता है। यह भारत श्रद्धा के
तौर पर ही संदर्भित हो- प्रवासी लेखन में ऐसा एक नियम की तरह
नहीं हुआ। लेकिन इस भारत में एक होम
रीडरशिप है, जिसका अवधान लेखन के
मन से कभी नहीं उतरता।
क्या प्रवासी साहित्य हिन्दी के अभिजन का, एलीट का साहित्य है?
हिंदी की लीज़र-क्लास का, विश्रांति-वर्ग का? जिसके लिए यह एक
फुरसत का शगल है? क्योंकि अब यह साहित्य अपना वर्ग-चरित्र
परिवर्तित कर चुका है। अब यह गिरमिटियों का साहित्य नहीं है।
अब उपनिवेशवाद के चलते लोग भारत से बाहर नहीं जाते, अब वे
वैश्वीकरण के चलते बाहर जाते हैं। इसलिए अब उन लोगों के सामने
वह स्थिति नहीं है जब झुंड के झुंड देश के बाहर मजदूरी के लिए
ठेल दिए जाते थे, अब तो व्यक्तिगत निर्वाचन के चलते प्रवास
होता है। फिर भी अचला शर्मा की ‘मेहरचंद की दुआ’ शीर्षक कहानी
अभी भी मजदूर वर्ग की कहानी है। यह एक दिलचस्प विषय हो सकता है
कि अपने औपनिवेशक देश में जाकर वहाँ रहते हुए आधुनिक भारत से
आए इस प्रवासी को कैसा लगता है। सत्येन्द्र श्रीवास्तव अपनी एक
कविता में कहते हैं- ‘‘सर विंस्टन आप मेरी मॉ को जानते है। वह
भी एक सात महीने के बच्चे का पेट फुलाए/मेरे पिता का आशीष
लेकर/मसूरी के उसी रास्ते पर लेट गई थी। जहाँ से फौजियों के
दस्तों को लौटना पडा था……/मैं उसी मां के पेट से जन्मा उसका
बेटा हूं। और मेरा नाम सत्येन्द्र है। और मैं आपसे यह कहने आया
हूँ कि मैं अब इंग्लैड में आ गया हूँ’’ यहाँ
औपनिवेशिक
दुःस्वप्न नए भारत के इस विश्व- नागरिक से टकराया गया है।
यह विश्व-नागरिक भारतीय सिर्फ यू.के/यू.एस.ए. ही नहीं जाता।
मध्यपूर्व भी जाता है और वहाँ वैश्वीकरण के दुःस्वप्नों से
भिड़ता है। तेजेन्द्र शर्मा की ‘ढ़िबरी टाइट’ में इसे देखिए।
अपनी करूणा में यह कहानी ‘उसने कहा था’ की याद दिलाती है।
इसलिए नहीं कि दोनों की पृष्ठभूमि पंजाबी है, इसलिए भी नहीं कि
दोनों में किसी ‘वार’ या ‘युद्ध’ की पृष्ठभूमि है, बल्कि इसलिए
कि दोनों में स्मृतियाँ हैं। गुंजित और प्रतिगुंजित होती हुई,
दोनों में निराशा है, फ़र्क़ है। एक में मृत्यु के ऊपर प्यार
की विजय है। एक में प्यार के ऊपर मृत्यु की विजय है। एक में
मूक कर देने वाला वाचाल प्यार है, दूसरे में मूक और स्तब्ध कर
देने वाली मृत्यु है। सैनिक का बलिदान है एक में, नागरिक की
बलि है दूसरे में। दोनों में आखि़री वाक्य एक टीस की रेख भीतर
की ज़मीन पर खींच जाता है। कुवैत पर ईराकी सेना का आक्रमण।
प्रकटतः असम्बद्ध। लेकिन अवसाद के आघात से ग्रस्त आदमी के लिए
वह एक बहुत दूरवर्ती से, बहुत कमजोर से दिखने वाले संबंध का
बहुत महीन तार भी जैसे किसी बड़ी हद तक एक अनुशोध है। एक आम
आदमी की आत्यन्तिक असहायता की सम्पूर्ण स्थापना है वह। न केवल
एक विदेशी परिवेश की असंवेदनशीलता के विरूद्ध बल्कि शायद
मृत्यु के देवता के समक्ष।
नियति के समक्ष।
मृत्यु तेजेन्द्र के यहाँ एक तरह की अतार्किकता है। वह तर्क और
विवेक का
ध्रुवान्त है। वहाँ मृत्यु की तत्वमीमांसा नहीं है। बस वहाँ है तर्क के विरूद्ध खुद को संभव करती हुई, एक
बिंदु की
तरह नहीं, एक प्रक्रिया की तरह, खिंची हुई, त्रिशंकु की तरह
टॅंगी हुई, बार-बार सामने आते हुए सवाल की तरह, एक संक्रमण
की तरह नहीं, एक संक्रामण की तरह,
व्यापती हुई- मृत्यु, कि जिसका कोई मापदण्ड नहीं है। ‘कैंसर’ नाम वाली कहानी को देखें या ‘देह
की कीमत’ को या उसी ‘ढिबरी टाइट’ को -तेजेन्द्र जैसे किसी
मृत्यु से लगातार तर्क कर रहे हैं, लेकिन मृत्यु जैसे अपने को
सदाचरित कर ही नहीं रही।
अपने वास्तविक जीवन में ज़िन्दगी से इतना प्यार करने वाले
तेजेन्द्र के यहाँ मृत्यु के बारे में इतनी अन्तर्दृष्टियाँ
मिलेंगी, यह शुरू-शुरू में मैं उम्मीद ही नहीं करता था। कैंसर
में यदि वह एक तरह की बायोलाजिकल फ्रीजिंग है तो ‘देह की कीमत’
में वह उतनी ही निर्मम है, जैसे ‘कफ़न’ में प्रेमचन्द के यहाँ।
जैसे कफ़न में गरीबी के कारण पनपी संवेदनहीनता है, वैसे ‘देह की कीमत’ में
आधुनिकता की दौर की संवेदनहीताएँ है। घीसू-माधव की तुलना में
ये ज्यादा त्रासद लगती हैं, क्योंकि इन्हें सही साबित करने के
लिए ग़रीबी का तर्क भी अनुपलब्ध है। केवल मृत्यु ही जीवन का
अतिक्रमण नहीं करती, कई बार जीवन भी मृत्यु का अतिक्रमण करता है।
और फिर ‘कैंसर’ तेजेन्द्र एक घायल कथाकार हैं। कैंसर पर
उनकी तीन कहानियाँ हैं। अपराधबोध का प्रेत, कैंसर और रेत का
घरौंदा। मुझे इन कहानियों को पढ़कर याद आई हैं कुछ और
कहानियाँ- ऐमी ग्रनबर्गर की ‘कीमोथिरेपी’, एड्रियन रिच की ‘अ
वुमैन डेड इन हर फोर्टीज’, जेम्स की डिकी की ‘द कैंसर मैच’ और
पैट्रेशिया गोएडिक की ‘इन दा हास्पिटल’ जैसी कहानियाँ- जो सबकी
सब कैंसर पर हैं। कैंसर की पृष्ठिभूमि इन कहानियों में होने का
एक आनुभविक कारण हो सकता हैं, लेकिन एक बड़ा कारण यह हैं कि
कैंसर के सामने मनुष्य की निरूपायता।
तेजेन्द्र की कहानियों में
जो एकाग्रता है, वह
भी शायद मृत्यु के उसी आसन्न स्वभाव का परिणाम है, दीवार
पर-सामने की दीवार पर-आने वाली विडंबना की तस्वीरें झूल रहीं
हैं और तेजेन्द्र उसे लिखते ही चले जा रहे हैं। उनका वश चले तो
समय को चूर-चूर कर दें, बस नहीं चलता। तो उस अनुभव को
पुनर्जीवित
कैसे किया जाए? एक कहानी लिखकर भी काम नहीं बनता इसलिए बार-बार
वे अलग-अलग तरह से उसे लिखते हैं। बीमारी जैसे हमारे शरीर में
नहीं, हमारे संबंधों में घर कर गई है। तो कैंसर संबंधो को
व्याख्यायित करता है। वह एक बीमारी की तरह नहीं उभरता, एक आईने
की तरह लगता हैं जिसमें
हर चेहरे, हर संबंध की सच्चाई सामने आ जाती हैं।
प्रवासी हिन्दी साहित्य का एक अध्ययन इस दृष्टि से होना शेष है
कि प्रवास के देश की तत्समय प्रचलित साहित्यिक शैलियों और
परंपराओं का कितना प्रभाव हिन्दी की प्रवासी रचनाओं पर पड़ा।
क्या वे कुछ ऐसे आयात हैं जिन्होंने हिन्दी को एक नई समृद्धि
दी? यानी प्रवासी हिन्दी साहित्यकार से हमारी अपेक्षा यह नहीं
है कि वह प्रवास के देश में अपने भाषाई सहधर्मियों का एक
अल्पसंख्यक समूह बना ले और उन्हीं गोष्ठियों में ग़ाफिल रहे
बल्कि यह कि अपनी नेचुरलाइज्ड कंट्री की सर्वश्रेष्ठ और आधुनिक
सृजन-प्रथाओं और मुहावरों को अपनी लेखन-प्रेरणाओं में, अपनी
रचना-रीति के फैब्रिक में स्थान दे। रचना-रीति से मेरा
अभिप्राय अभिव्यक्ति के नखरों से नहीं है बल्कि एक तरह के विजन
से है। अलबत्ता अल्पसंख्यक होने का जो एक अहसास है, उसकी एक
प्रामाणिक अभिव्यक्ति जरूर प्रवासी लेखक अपने साहित्य में कर
सकते हैं। यदि वे ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो इसके पीछे उनकी
पृष्ठभूमि से आ रही रौशनी ही है। इस कारण वे हमेशा भारत के
बहुल से सम्पृक्त महसूस करते हैं और कभी अल्पता- बोध से ग्रस्त
नहीं होते।
पूर्णिमा वर्मन ने अपनी कहानी ‘यों ही चलते हुए’
में इसे यों निष्पत्ति दी है: शायद हर भारतीय का यही तरीका है-
वे या तो अपने चौखाने पार नहीं करते या हजारों चौखाने पार करते
हुए अपने चौखानों पर वापस लौट आते हैं। शायद इसीलिए दुनिया में
कहीं भी रहें चौखानों की भीड़ में वे खोते नहीं। हर बार मेन
रोड पर मिल जाते हैं…जिन्दगी में भी। वे हिंदी में लिख रहे
हैं, यही इस बात का सबूत है कि सांस्कृतिक वैभिन्य से अभी
उन्होंने संकोच नहीं किया है। उनका लेखन उनके अस्तित्व की एक
सहवर्ती (साइमल्टेनियस) उपलब्धि है। जड़ से उखड़ना एक अनुभव
है। कृष्ण बिहारी की कहानी जड़ों से कटने पर में कथाकार का
निष्कर्ष है कि ‘पहली बार अहसास हुआ कि अपने देश के अंदर आदमी
की अपनी और जड़ों की जो ताकत होती है वह दूसरे देश में कोई
औकात नहीं रखती। लेकिन उसके साथ साथ एक अनुभव हवा में तैरने का भी है। अब इस फ्लोटिंग को आप प्रेम जनमेजय
की कहानी क्षितिज पर उड़ती स्कारलेट आयबिस के रूप में देखें जो
त्रिनिदाद का राष्ट्रीय पक्षी है-कहानीकार के शब्दों में- नीले
आसमान में कहीं भी जाने को स्वतंत्र पंख पसारता। गौतम सचदेव की
कहानी आकाश की बेटी जिसमें व्हील चेयर से बंधी स्त्री कत्थई
कबूतरी का इंतजार करते हुए आकाश की ओर देख रही है भी शायद इसी
द्वैत की कहानी है। प्रवासी लेखन की इस दोहर में ही उसकी
अद्वितीयता है।
४
अप्रैल
२०११ |