|
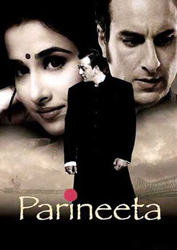 1 1
हिंदी सिनेमा कितना हिंदी
-विनोद अनुपम
श्यामा कुमार इंग्लैंड में
रहती हैं, हिंदी में कविताएँ लिखती हैं, इनके पति डॉ
अंजनी कुमार कहने को बीस वर्षों से वहीं हैं, लेकिन उनकी
जड़ें अभी भी भारत में ही हैं। इंग्लैंड में अपनी सीमाभर
हिंदी का अलख उन्होंने जगाए रखा है, हिंदी प्रसार के
कुछेक आंदोलनों से भी जुड़े हैं। वे कहते हैं, मेरी पहली
कोशिश होती है कि हम भारतीय जहाँ भी - जब भी वहाँ मिलें
तो हिंदी में ही बातें करें।
करते भी हैं, लेकिन मुश्किल घर में ही होती है,
बच्चे इंग्लैंड में ही पैदा हुए, वहीं पले-बढ़े, वे अंग्रेज़ी में अधिक सहज हैं।
इसका निदान ढूँढ़ने की कोशिश में डॉ दंपत्ति ने घर में हिंदी फ़िल्मों का ज़खीरा
जमा कर लिया, 'मुगल-ए-आजम' से लेकर 'आज का अर्जुन' तक। रूस के हिंदी विद्वान
बारान्निकोव की तरह उन्हें भी उम्मीद थी कि हिंदी फ़िल्मों को देखते हुए बच्चे
हिंदी को स्वीकार भी कर लेंगे और उसमें सहज भी हो जाएँगे। उनकी आशा के अनुरूप बच्चे
हिंदी सिनेमा देखते भी हैं, पसंद भी करते हैं लेकिन हिंदी में बात करने के लिए
प्रेरित करने पर कहते हैं, 'यह ज़रूरी है क्या! जब हिंदी फ़िल्म में काम करने वाले
कलाकारों को हिंदी में बात करने की ज़रूरत नहीं होती तो हम देखने वालों को क्यों
होगी? डॉ दंपत्ति के पास कोई जवाब नहीं होता। वे शून्य में एक सवाल उछालते हैं,
'आख़िर हिंदी फ़िल्मों के कलाकार हिंदी के विस्तार या विकास की जवाबदेही क्यों नहीं
महसूस करते?'
वास्तव में ऐसा लगता है हिंदी फ़िल्म जगत के लिए
हिंदी सिर्फ़ परदे पर की भाषा है। हतप्रभ रह जाना पड़ता है जब 'लगान' में अवधी
बोलने वाले आमिर खान टेलीविजन पर दर्शकों से ये कहते हुए रू-ब-रू होते हैं, 'मैं
अंग्रेज़ी में अधिक 'कंफर्टेबल' महसूस करता हूँ।' आमिर खान ही क्यों, शाहरुख खान से
लेकर अवसर की आस में टोह लगाए नवोदित कलाकारों तक सभी की कोशिश होती है, टेलीविजन
पर जब भी दिखें अंग्रेज़ी बोलते ही। आज भूमिका के बाहर शायद ही कोई कलाकार हिंदी का
व्यवहार करता दिखता हो, ऐसा लगता है अभिनय के साथ हिंदी बोलने की भी कीमत लेते हैं
हमारे कलाकार। आमिर खान के पास तो ऑस्कर पाने का सबक था, इन कलाकारों के सामने
अंग्रेज़ी में बात करने की कौन-सी बाध्यता हो सकती है, यह समझ से परे है। सबसे दुखद
तब महसूस होता है जब साक्षात्कार लेने वाले के हिंदी में जवाब देने के आग्रह पर भी
वे हिंदी में बात करने की ज़रूरत महसूस नहीं करते।
यहाँ अमिताभ बच्चन को अपवाद मान सकते हैं, जो अपनी साहित्यिक विरासत का सम्मान करते
हुए ज़रूरत पड़ने पर परदे के बाहर भी सहज और संप्रेष्य हिंदी का व्यवहार करते हैं।
गोविंदा ने शुरू से ही अपनी छवि भदेस कलाकार की बनाई है, आम जनता की पसंद को
प्रतिबिंबित करते गोविंदा भी कभी अंग्रेज़ी का व्यवहार करते नहीं दिखते। हिंदी से
भावनात्मक लगाव रखने वाले आशुतोष राणा जैसे कलाकार भी हिंदी सिनेमा में हैं, लेकिन
अंग्रेज़ीदां कलाकारों के सामने इनकी संख्या इतनी छोटी है कि हिंदी बोलने वाले
हिंदी फ़िल्म कलाकारों की कोई अलग पहचान ही नहीं बन पाती। यहाँ ऐश्वर्या राय का
उल्लेख आवश्यक है जिन्होंने अपनी अंतर्राष्ट्रीय छवि के बावजूद हिंदी में पूछे गए
सवालों का जवाब हिंदी में देने का निश्चय किया है। ऐश्वर्या का यह निश्चय ख़बर बनती
है, आश्चर्य है कमल हसन या रजनीकांत का तमिल बोलना ख़बर नहीं बनता, कोई रूसी या
जापानी कलाकार अपनी मूल भाषा नहीं बोले तो ख़बर वह बनती है, लेकिन हिंदी कलाकार
हिंदी बोल ले, तो ख़बर वह बनती है।
वास्तव में टेलीविजन के फैलाए संजाल ने संस्कृति
में अपने जो भी सार्थक-निरर्थक हस्तक्षेप दिखाए, उनमें एक यह भी है। पहले कलाकारों
से सामना दर्शकों को सिर्फ़ सिनेमा के परदे पर होता था, बाकी पत्र-पत्रिकाओं में
उनके गॉसिप्स हम पढ़ भले ही लें, उन्हें देखना संभव नहीं हो पाता था। परदे पर तो
पात्रों के रूप में कलाकारों का नायकत्व हम सहज स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन इस
'नायक' की छवि परदे के बाहर भी उनके साथ जुड़ी रहे, अब कलाकारों की यह चिंताएँ बनी
रहती हैं। इसके लिए एक सबसे आसान रास्ता दिखता है उन्हें आम जनता की भाषा से दूरी
बनाए रखने का, जिसकी परंपरा राजनीतिज्ञों ने आज़ादी के बाद ही शुरू कर दी थी। उनकी
कोशिश जनता को यह जताने की होती है कि पात्र के रूप में हिंदी बोलकर मैं एहसान कर
रहा हूँ तुम लोगों पर। वास्तव में तो मैं पात्रों से भी महान हूँ। अपनी इस 'स्टार
छवि' के प्रति जो कलाकार जितना ही सचेत रहता है, वह आम जनता से उतनी ही दूरी बनाए
रखने की कोशिश करता है। पता है उसे सितारों की चमक दूरी पर ही निर्भर करती है।
कलाकारों को हिंदी की संप्रेषणीयता पर ही संदेह हो, यह तो माना ही नहीं जा सकता,
हिंदी फ़िल्मकारों को यह तो अहसास है कि वे सर्वाधिक पहुँच वाली फ़िल्मों में काम
कर रहे हैं। उन्हें पता है कि हिंदुस्तान के सबसे महँगे कलाकार रजनीकांत हों या
प्रतिभाशाली कमल हसन हिंदी में काम करने की इच्छा से मुक्त नहीं हो पाते। मणिरत्नम
और प्रियदर्शन जैसे फ़िल्मकार को भी अपनी पूर्णता ज़ाहिर करने के लिए हिंदी का ही
सहारा लेना पड़ता है।
लेकिन यह हिंदी सिनेमा के व्यवसाय बुद्धि की
पराकाष्ठा ही है कि यहाँ हिंदी बस वहीं तक स्वीकार्य है, जहाँ तक अनिवार्य है। कोई
भी भाषा-भाषी यह देख चकित रह जा सकती है कि हिंदी सिनेमा की नामावली हिंदी में देने
की कोई अनिवार्यता नहीं समझी जाती। अधिकांश ही नहीं, शत-प्रतिशत हिंदी सिनेमा की
नामावली में प्रमुखता से अंग्रेज़ी में नाम दिया जाता है, फिर हिंदी या उर्दू में
लगभग साथ-साथ नाम आते हैं। फिर बाकी की नामावली सिर्फ़ अंग्रेज़ी में चलती है।
अपवाद में सिर्फ़ 'राजश्री प्रोडक्शन' का नाम लिया जा सकता है, जिसने अपनी छियालीस
फ़िल्मों तक हिंदी में नामावली देने की परंपरा का निर्वाह ही नहीं किया बल्कि अपनी
फ़िल्मों में भी हिंदी समाज, सभ्यता, संस्कृति को स्थापित करने-प्रदर्शित करने की
सफल कोशिश की। लेकिन अपनी छियालिस सफल फ़िल्मों की लंबी परंपरा के बाद शायद राजश्री
को भी 'ग़लती' का अहसास हुआ, तब जब राजश्री के संस्थापक ताराचंद बड़जात्या के पौत्र
सूरज बड़जात्या अमेरिका से फ़िल्ममेकिंग सीखकर आते हैं, पता नहीं अमेरिका में
फ़िल्म मेकिंग सीखने के दौरान अमेरिका से वे अपनी भाषा के प्रति लगाव क्यों नहीं
सीख पाते! सूरज के 'राजश्री' का कमान सँभालने के बाद, पहली ही फ़िल्म 'मैंने प्यार
किया' के साथ वे मुख्यधारा के 'नियमों' को स्वीकार करते अंग्रेज़ी ही नहीं,
अंग्रेज़ियत भी स्वीकार करते दिखते हैं। आश्चर्य नहीं कि 'आरती' और 'दोस्ती' जैसी
फ़िल्मों से शुरू होने वाली राजश्री अपनी पचासवीं फ़िल्म के रूप में 'मैं प्रेम की
दिवानी हूँ' प्रस्तुत करती हैं जिसमें हिंदी के साथ-साथ हिंदी संस्कृति के प्रति भी
पूर्णतया परहेज़ देखा जा सकता है।
एक छोटा-सा वाकया, दक्षिण भारतीय फ़िल्मकार जीवा
अपनी एक चर्चित प्रेमकथा का रिमेक हिंदी में बनाते हैं, फ़िल्म का नाम होता है
'रण'। कहानी अपने प्रेम को पाने के लिए नायक द्वारा कई मोर्चे पर लड़ी जाने वाली
लड़ाइयों की है। इससे बेहतर नाम हिंदी में सोचा भी नहीं जा सकता था, लेकिन समस्या आ
गई, फ़िल्म के पोस्टर तो अंग्रेज़ी में बनने थे, प्रचार सामग्रियाँ अंग्रेज़ी में
छपनी थी। फ़िल्म की नामवली अंग्रेज़ी में आनी थी। रण लिखा कैसे जाय? आर. यू. एन.
लिखते हैं तो 'रन' हो जाता है, मतलब दौड़। इस दौड़ और रण की क्या समानता हो सकती
है? लेकिन फ़िल्म का नाम बदल दिया जाता है। जीवा फ़िल्म का नाम बदलना स्वीकार कर
लेते हैं लेकिन अंग्रेज़ी का मोह नहीं छोड़ पाते, 'रण' अपने निरर्थक से नाम 'रन' के
साथ प्रदर्शित होती है।
हमारे फ़िल्मकारों में समझ-बूझकर गल़त स्वीकार
करने की हिम्मत इसलिए है कि हम खुद ही अपनी भाषा के प्रति उदासीन हैं। हिंदी भाषी
लोगों की ओर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हिंदी के साथ कितना खिलवाड़ किया जा रहा
है। यही कारण है कि पोस्टरों और प्रचार सामग्रियों में हिंदी की शुद्धता के प्रति
कतई चिंता नहीं की जाती। रोज़-रोज़ अवतरित हो रहे सिनेमा के पोस्टरों से यदि हिंदी
के 'विलक्षण' शब्द संयोजनों को इकठ्ठा करना शुरू कर दें तो वह एक नया थिसारस बन
सकता है।
यश चोपड़ा जैसे प्रतिष्ठित फ़िल्मकार 'मोहब्बतें'
बनाते हैं, करोड़ो खर्च कर, लेकिन सौ रुपए खर्च कर एक व्याकरण के जानकार की मदद
नहीं ले सकते। मोहब्बत भाववाचक संज्ञा है, जिसके बहुवचन व्यवहार में नहीं आते।
लेकिन यह सोचने की ज़रूरत क्या है, दर्शकों को हिंदी नहीं चाहिए, अमिताभ चाहिए,
ऐश्वर्या चाहिए, शाहरुख चाहिए। हिंदी के प्रति सिनेमा का यह तात्कालिक नज़रिया ही
वह कारण है जो भाषा के विकास में यह अपनी क्षमता भर योगदान देने में सफल नहीं हो
सका। वास्तव में हिंदी क्या सिर्फ़ हिंदी होती है। क्षणभर ठहरकर सोचें भाषा एक
भरी-पूरी संस्कृति की वाहक होती है। अन्यथा नहीं कि भाषा के प्रति खिलवाड़ की
स्वीकार्यता ने ही फ़िल्मकारों को यह हिम्मत दी है कि वे आज हमारी संस्कृति से भी
खिलवाड़ करने को तैयार हैं।
विनोद भारद्वाज स्पष्ट शब्दों में लिखते हैं, 'अभी
तक हिंदी सिनेमा के नाम पर जो फ़िल्में बनी हैं वो कहने को ही हिंदी हैं। श्याम
बेनेगल की फ़िल्मों में चित्रित परिवेश आमतौर से गुजरात, महाराष्ट्र या आंध्र
प्रदेश का है। कुमार साहनी या मणिकौल ने जो फ़िल्में बनाई हैं, उनका संबंध एक दूसरी
तरह के परिवेश से है। यथार्थ को वे दूसरी तरह से परिभाषित करते रहे हैं। मृणाल सेन
की हिंदी फ़िल्मों में उत्तर भारत का परिवेश आपको नहीं मिलेगा। सईद मिर्ज़ा जैसे
फ़िल्मकार अपनी फ़िल्मों में मुंबई की ज़िंदगी को आधार बना रहे हैं, क्यों कि उसी
जीवन को वे जानते हैं। स्पष्ट है इन सब फ़िल्मकारों ने अपेक्षाकृत बड़ा वर्ग
प्राप्त करने के लिए ही हिंदी या हिंदुस्तानी का इस्तेमाल किया है। पीलीभीत या
राजनांदगाँव का यथार्थ जब किसी फ़िल्मकार ने देखा ही नहीं है, तो सिनेमा में वह
यथार्थ हमें दिखेगा कैसे?'
वास्तव में मणिरत्नम को हिंदी नहीं आती, लेकिन
'रोज़ा' और 'बांबे' की सफलता से उत्साहित वे हिंदी में अपनी पहली फ़िल्म 'दिल से'
बनाना तय करते हैं। फिर 'युवा' भी बनाते हैं, बिना हिंदी सीखे। फ़िल्म की पटकथा
अंग्रेज़ी में लिखी जाती है। सत्यजीत राय प्रतिष्ठा की पराकाष्ठा पर पहुँचकर हिंदी
में फ़िल्म बनाने के लिए प्रेमचंद की कहानी 'शतरंज के खिलाड़ी' का चयन करते हैं
फ़िल्म की पटकथा ही अंग्रेज़ी में तैयार नहीं होती, संवाद तक रोमन में लिखे जाते
हैं। 'शोले' और 'दीवार' जैसी फ़िल्मों के लेखन जावेद अख़्तर यह कहने में ज़रा-सा
नहीं संकोच करते कि मैंने हिंदी कभी पढ़ी नहीं और इसे लिख नहीं सकता। वे कहते हैं,
पटकथा मूलरूप से तो अंग्रेज़ी में ही लिखी जाती है, बाद में संवादों का हिंदी या
उर्दू में तर्जुमा किया जाता है। आश्चर्य नहीं कि पटकथा के इस अनुशासन का पालन उदय
प्रकाश जैसे हिंदी के प्रतिष्ठित युवा साहित्यकार भी करते हैं। वे भी पटकथा हिंदी
में लिखने की ज़हमत नहीं उठाते। अंग्रेज़ी की बुनियाद पर खड़ी होने वाली हिंदी
सिनेमा यदि अपने समाज, अपनी जाति, अपनी भाषा, अपने लोग, अपनी संस्कृति से नहीं जुड़
पाती है तो इसमें आश्चर्य क्या है।
यहाँ पर प्रकाश झा का उल्लेख आवश्यक है, जिन्हें
हिंदी का फ़िल्मकार, शायद एकमात्र फ़िल्मकार कहने का जोखिम उठाया जा सकता है। अपनी
पहली फ़िल्म के लिए वे शैवाल की कहानी का चुनाव करते हैं, शैवाल से ही पटकथा-संवाद
लिखवाते हैं और 'दामुल' तैयार होती है। मूलरूप में पटकथा हिंदी में लिखी जाती है,
और बिहार के गाँवों के अंधेरे को पूरी ताकत से यह बयान करती है। बिहार में तो ख़ैर
प्रकाश झा और शैवाल के अपने अनुभव हो सकते हैं, लेकिन यही प्रकाश झा राजस्थान की
पृष्ठभूमि पर फ़िल्माने के लिए विजयदान देश की कहानी 'परिणति' का चुनाव करते हैं,
तो परदे पर उभरती राजस्थानी संस्कृति की पूर्णता शायद ही कभी सवाल खड़े करने का
अवसर देती है। वास्तव में किसी भी भाषा और संस्कृति को 'जानने' से अधिक महत्वपूर्ण
उसे स्वीकार करना है। फ़िल्मकारों के साथ मुश्किल है कि वे न तो हिंदी जानते हैं, न
ही उसे स्वीकार करना चाहते हैं।
हिंदी भाषा के प्रति सिनेमा का यह नज़रिया दुखद
भले हो, अस्वाभाविक नहीं। छत्तीसगढ़ी सिनेमा छत्तीसगढ़ में विकसित हो रही है,
उड़ीसा में उड़िया, बंगाल में बंगला सिनेमा, असम में असमिया, मलयालम सिनेमा केरल
में विकसित हुई, लेकिन हिंदी सिनेमा को ज़मीन मिली एक ग़ैर हिंदी भाषी प्रांत
महाराष्ट्र में। अपने-अपने प्रदेशों में विकसित होकर भारत में जहाँ क्षेत्रीय
सिनेमाओं ने विकसित होकर अंतर्राष्ट्रीय पहचान दर्ज़ की, वही हिंदी सिनेमा मूलरूप
से 'बाज़ार' की वस्तु बनकर रह गया, बगैर किसी सांस्कृतिक पहचान के।
वास्तव में भारत में सिनेमा के आरंभिक दौर में ही
हिंदी को स्वीकार्य करने की एकमात्र वजह इसकी अधिसंख्य लोगों तक पहुँच थी, जानने-ना
जानने के बावजूद अधिसंख्य क्षेत्रों में इसकी सहज संप्रेषणीयता थी। हिंदी की इसी
क्षमता ने भारत में सिनेमा की मुख्यधारा जो मुंबई में गठित हुई थी, को हिंदी पर
आश्रित रखा, हिंदी के प्रति कोई सम्मान या श्रद्धा ने नहीं। पूँजी उनके पास थी,
हिंदी उनके लिए मात्र ज़रूरत की भाषा थी। अफ़सोस यह कि हिंदी सिनेमा से जुड़े
अहिंदी-भाषियों की बात तो छोड़ ही दें, हिंदी क्षेत्र से गए लोगों ने भी हिंदी
सिनेमा में हिंदी की प्रतिष्ठा को बहाल करने की कोई संगठित कोशिश नहीं की। हिंदी
में 'बड़ी' फ़िल्म बनाना सोचा जाता है तो बंगाल से दसियों बार फ़िल्माया गया
क्लासिक ढूंढ़कर लाया जाता है, जिस तरह हिंदी सिनेमा पूरे देश का प्रतिनिधित्व करती
है, इसमें कुछ बेजा है भी नहीं। लेकिन जिस तरह हिंदी की विपुल साहित्य संपदा को
सिनेमा नज़रअंदाज़ करती रही है, स्पष्ट लगता है यह स्वाभाविक नहीं। 'गोदान' से लेकर
'ढलान' तक और 'गुनाहों का देवता' से लेकर 'कसम' तक कहीं कोई सिनेमाई संभावना हिंदी
फ़िल्मकारों को आकर्षित नहीं कर पाती, वह भी तब, जब 'तीसरी कसम' जैसी कालजयी
फ़िल्में उनके सामने हों। कैसा है यह हिंदी का सिनेमा! क्या ज़रूरत नहीं लगती कि
हिंदी क्षेत्रों को भी अब 'अपना' सिनेमा विकसित करने की कोशिश करनी चाहिए? हमें
'लगान' तो चाहिए, 'देवदास' भी लेकिन 'गोदान' भी और 'मुझे चाँद चाहिए' भी।
९ फरवरी २००६
|