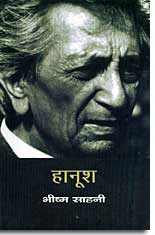
1
''हानूश'' का जन्म
भीष्म साहनी
''हानूश'' नाटक की प्रेरणा
मुझे चेकोस्लोवेकिया की राजधानी प्राग से मिली। यूरोप की
यात्रा करते हुए एक बार शीला और मैं प्राग पहुँचे। उन दिनों
निर्मल वर्मा वहीं पर थे। होटल में सामान रखने के फौरन ही
बाद मैं उनकी खोज में निकल पड़ा। उस हॉस्टल में जा पहुँचा
जिसका पता पहले से मेरे पास था। कमरा तो मैंने ढूँढ़ निकाला,
पर पता चला कि निर्मल वहाँ पर नहीं हैं। संभवतः वह इटली की
यात्रा पर गए हुए थे। बड़ी निराशा हुई। पर अचानक ही, दुसरे
दिन वह पहुँच भी गए और फिर उनके साथ उन सभी विरल स्मारकों,
गिरजा स्थलों को देखने का सुअवसर मिला, विशेषकर गॉथिक और
'बरोक' गिरजाघरों को जिनकी निर्मल को गहरी जानकारी थी।
और इसी धुमक्कड़ी में हमने
हानूश की घड़ी देखी। यह मीनारी घड़ी प्राग की नगरपालिका पर
सैंकड़ों वर्ष पहले लगाई गई थी, चेकोस्लोवेकिया में बनाई
जानेवाली पहली मीनारी घड़ी मानी जाती थी। उसके साथ एक दंतकथा
जुड़ी थी कि उसे बनानेवाला एक साधारण कुफ़लसाज था कि उसे
घड़ी बनाने में सत्रह साल लग गए और जब वह बन कर तैयार हुई तो
राजा ने उसे अंधा करवा दिया ताकि वह ऐसी कोई दूसरी घड़ी न
बना सके। घड़ी को दिखाते हुए निर्मल ने इससे जुड़ी वह कथा भी
सुनाई। सुनते ही मुझे लगा कि इस कथा में बड़े नाटकीय तत्व
हैं, कि यह नाटक का रूप ले सकती है।
यूरोप की यात्रा के बाद
मॉस्को लौटने पर मैं कुछ ही दिन बाद, चेकोस्लोवेकिया के
इतावाद (मॉस्को स्थित) में जा पहुँचा। सांस्कृतिक मामलों के
सचिव से, हानूश की दीवारी घड़ी की चर्चा और अनुरोध किया कि
उसके संबंध में यदि कुछ सामग्री उपलब्ध हो सके तो मैं आभार
मानूँगा। लगभग एक महीने बाद दूतावास से टेलीफ़ोन आया कि आकर
मिलो। मैं भागता हुआ जो पहुँचा। अधिक सामग्री तो नहीं मिली
पर किसी पत्रिका में प्रकाशित एक लेख ज़रूर मिला। मैं लेख की
प्रति ले आया, पर लेख चेक भाषा में था।
सौभाग्यवश मेरे पत्रकार
मित्र, मसऊद अली खान की पत्नी कात्या, चेकोस्लोवेकिया की
रहने वाली थी। उन्होंने झट से उसका अंग्रेज़ी में अनुवाद कर
डाला। मुझे नाटक लिखने के लिए आधार मिल गया और वह दो पन्नों
का आधार ही मेरे पास था। जब मैं भारत लौटा वे १९६३ के दिन
थे। नाटक के लिखे जाने और खेले जाने में अभी बहुत वक्त था।
और इसकी अपनी कहानी है। अंततः नाटक १९७७ में खेला गया।
हानूश नाटक पर मैं लंबे
अर्से तक काम करता रहा था। पहली बार जब नाटक की पांडुलिपि
तैयार हुई तो मैं उसे लेकर मुंबई जा पहुँचा बलराज जी को
दिखाने के लिए। उन्होंने पढ़ा और ढ़ेरों ठंडा पानी मेरे सिर
पर उड़ेल दिया। ''नाटक लिखना तुम्हारे बस का नहीं है।''
उन्होंने ये शब्द कहे तो नहीं पर उनका अभिप्राय यही था। उनके
चेहरे पर हमदर्दी का भाव भी यही कह रहा था।
पर मैं हतोत्साह नहीं हुआ।
घर लौट आया। उसे कुछ दिन ताक पर रखा, पर फिर उठाकर उस पर काम
करने लगा और कुछ अर्सा बाद नाटक की संशोधित पांडुलिपि लिए
उनके पास फिर जा पहुँचा। उन्होंने पढ़ा और फिर सिर हिला
दिया। उनका ढ़ाढस बँधाने का अंदाज़ भी कुछ ऐसा था कि यह काम
तुम्हारे बस का नहीं है। इस पचड़े में से निकल आओ।
उनकी प्रतिक्रिया सुनते हुए
मुझे संस्कृत की एक दृष्टांत-कथा याद हो आई जिसे बचपन में
सुना था। एक गीदड़ अपने दोस्तों के सामने डींग हाँक रहा था
कि शेर को मारने क्यों मुश्किल है। बस, आँखें लाल होनी चाहिए,
मूँछ ऐंठी हुई और पूँछ तनी हुई, शेर आए तो एक ही झपट्टे में
उसे चित कर दो। . . .वह कह ही रहा था कि उधर से शेर आ गया।
बाकी गीदड़ तो इधर-उधर भाग गए पर यह गीदड़ शेर से दो-चार
होने के लिए तैयारी करने लगा। वह मूँछें ऐंठ रहा था जब शेर
पास आ पहुँचा और गीदड़ को एक झापड़ दिया कि गीदड़ लुढ़कता
हुआ दूर तक जा गिरा. . .जब गीदड़ फिर से इकठ्ठा हुए तो गीदड़
अपनी सफ़ाई देते हुए बोला, ''और सब तो ठीक था पर मेरी आँखें
ज़्यादा लाल नहीं हो पाई थीं, मूँछों में ज़्यादा ऐंठ भी
नहीं आई थी।'' पास में खड़ा एक बूढ़ा गीदड़ भी सुन रहा था।
गीदड़ को समझाते हुए बोला,
''शूरोऽसि कृत विद्योऽसि, दर्शनीयोऽसि पुत्रक,
यस्मिन् कुले त्वमुत्पन्नः सिंहस्तत्र न हन्यते।''
(बेटा, तुम बड़े शूरवीर हो, बड़े ज्ञानी हो, सभी दाँवपेंच
जानते हो, पर जिस कुल में तुम पैदा हुए हो, उस में शेर नहीं
मारे जाते।)
मैं अपना-सा मुँह लेकर दिल्ली लौट आया।
अब मैं बलराज जी की बात कैसे नहीं मानता। उनके निष्कर्ष के
पीछे 'इप्टा' के मंच का वर्षों का अनुभव था, फिर फ़िल्मों का
अनुभव।
मेरे अपने प्रयासों में भी
त्रुटियाँ रही थीं। ''हानूश'' का कथानक तो मुझे बाँधता था,
पर उसे नाटक में कैसे ढ़ालूँ, मेरे लिए कठिन हो रहा था। पहले
भी बार-बार कुछ लिखता रहा था। फिर निराश होकर छोड़ देता रहा
था। न छोड़े बनता था, न लिखते बनता था। ऐसा अनुभव शायद हर
लेखक को होता है। एक बार कीड़ा दिमाग़ में घुस जाए तो निकाले
नहीं निकलता। हर दूसरे महीने मैं उसे फिर से उठा लेता। कथानक
के नाम पर मेरे पास गिने-चुने ही तथ्य थे। नाटक का सारा
ताना-बाना मुझे बुनना था। कथानक की पृष्ठभूमि ऐतिहासिक थी और
वह भी मध्ययुगीन यूरोप की चेकोस्लोवेकिया की। मेरे अपने देश
की भी नहीं।
कुछ अरसा बाद नाटक की एक और
संशोधित पांडुलिपि तैयार हुई। या यों कहूँ एक और पांडुलिपि
तैयार हुई। अबकी बार मैं उसे बलराज जी के पास नहीं ले गया।
नाटक की टंकित प्रति उठाए मैं सीधा अलकाजी साहिब के पास
पहुँचा जो उन दिनों राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के निर्देशक
थे। मैंने बड़ी विनम्रता से अनुनय-विनय के साथ कहा, ''यदि आप
इसे एक नज़र देख जाएँ। मैं आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहता
हूँ।''
वह मुस्कराए। अलकाजी उन दिनों मुझे इतना भर जानते थे कि मैं
बलराज का भाई हूँ। बलराज के साथ मुंबई में रहते हुए उनके साथ
थोड़ा संपर्क रहा था।
उन्होंने नाटक की प्रति रख
ली और मैं बड़ा हल्का-फुल्का महसूस करता हुआ लौट आया। अब कुछ
तो पता चलेगा, मैंने मन ही मन कहा।
उसके बाद सप्ताह भर तो मैं शांत रहा, उसके बाद मेरी उत्सुकता
और मेरा इंतज़ार बढ़ने लगा। हर सुबह उठने पर यही सोचूँ, अब
अलकाजी साहिब ने पढ़ लिया होगा, अब तक ज़रूर पढ़ लिया होगा,
उन्हें टेलीफ़ोन कर के पूछूँ? नहीं, नहीं अभी नहीं मुझे
जल्दबाज़ी नहीं करनी चाहिए। मैं बड़ी बेसब्री से उनकी
प्रतिक्रिया का इंतज़ार कर रहा था।
दो सप्ताह बीत गए, फिर तीन, फिर चार, महीना भर गुज़र गया।
फिर डेढ़ महीना। मेरे मन में खीझ-सी उठने लगी। ऐसा भी क्या
है, मुझे बता सकते थे, टेलीफ़ोन कर सकते थे। इस चुप्पी से
क्या समझूँ?
जब दो महीने बीत गए तो
मुझसे नहीं रहा गया। मैं एक दिन सीधा राष्ट्रीय नाट्य
विद्यालय जा पहुँचा।
मैंने अपने नाम की 'चिट' अंदर भेजी। चपरासी अंदर छोड़ कर
बाहर निकल आया।
मैं बाहर बरामदे में खड़ा
इंतज़ार करता रहा। कोई जवाब नहीं, मुझे इतना भी मालूम नहीं
था कि अलकाजी साहिब दफ़तर में हैं भी या नहीं। वास्तव में
वह दफ़तर में नहीं थे। वह उस समय क्लास ले रहे थे। हमारे
यहाँ चपरासियों की बेरुखी भी समझ में आती हैं, वे यही मानकर
चलते हैं कि साहिब के पास 'चिट' भेजनेवाला आदमी नौकरी माँगने
आया है। उस समय मुझे इस बात का भी ध्यान नहीं आया कि
राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में भी क्लासें लगती होंगी। मैं
समझ बैठा था कि नाट्य विद्यालय में क्लासों का क्या काम,
वहाँ केवल रिहर्सलें होती होंगी।
मैंने फिर से एक 'चिट' भेजी
और चपरासी से ताक़ीद की कि यह बहुत ज़रूरी है, जहाँ भी
अलकाजी साहिब हों उन्हें देकर आओ।
मैं अपमानित-सा महसूस करने लगा था। अलकाजी साहिब की बेरुखी
पर झुँझलाने लगा था। मैंने ऐसा कौन-सा गुनाह किया था कि
मुझसे मिलने तक की उन्हें फ़ुर्सत नहीं थी।
इतने में देखा, अलकाजी साहिब बरामदे में चले आ रहे थे। आँखों
पर चश्मा, हाथ में खुली किताब।
''मैं क्लास ले रहा था। आप थोड़ा इंतज़ार कर लेते।'' मुझे
लगा रुखाई से बोल रहे हैं। वास्तव में उन्हें मेरा क्लास में
'चिट' भेजना नागवार गुज़रा था।
''मैं अपने नाटक के बारे में पूछने आया था।''
''वह मैं अभी पढ़ नहीं पाया। इस सेशन में काम बहुत रहता
है।''
किताब अभी भी उनके हाथ में
थी और वह थोड़ा उद्विग्न से चश्मों में से मेरी ओर देख रहे
थे, मानो क्लास में लौटने की जल्दी में हों।
तभी मैंने छूटते ही कहा!
''क्या मैं अपना नाटक वापस ले सकता हूँ।''
वह ठिठके। मेरी ओर कुछ देर
तक देखते रहे और फिर क्लास की ओर जाने के बजाय, अपने दफ़तर
का दरवाज़ा खोल कर अंदर चले गए और कुछ ही देर बाद नाटक की
प्रति उठाए चले आए और मेरे हाथ में देते हुए, बिना कुछ कहे,
क्लास रूम की ओर घूम गए।
मैंने घर लौट कर नाटक को
मेज़ पर पटक दिया। मारो गोली, यह काम सचमुच मेरे वश का नहीं
है।
दिन बीतने लगे। पर कुछ समय बाद फिर से मेरे दिल में
धुकधुकी-सी होने लगी। अलकाजी साहिब ने इसके पन्ने पलटना तक
गवारा नहीं किया। नहीं, नहीं पन्ने पलटे होंगे, नाटक बे सिर
पैर का लगा होगा तो उसे रख दिया कि कभी फ़ुर्सत से पढ़
लेंगे। मैंने मन ही मन कहा- अब मैं नाटक का मुँह नहीं
देखूँगा। बलराज ठीक ही कहते होंगे कि यह मेरे वश का रोग नहीं
है।
फिर एक दिन यह संभवतः
१९७६
के जाड़ों के दिन थे, शीला और मैं बुद्ध-जयंती बाग में टहल
रहे थे जब कुछ ही दूरी पर मुझे राजिंदर नाथ और सांत्वना जी
बाग में टहलते नज़र आए। राजिंदर नाथ जाने-माने निर्देशक थे।
जब पास से गुज़रे और दुआ-सलाम हुई तो मैंने कहा!
''यार मैंने एक नाटक लिखा है। वक्त हो तो उसे एक नज़र देख
जाओ।''
राजिंदर नाथ हँस पड़े। कहने लगे,
''मैं खुद इन दिनों किसी स्क्रिप्ट की तलाश में हूँ, कुछ ही
देर बाद राष्ट्रीय नाट्य समारोह होने जा रहा है।''
नेकी और पूछ-पूछ। मैंने नाटक की प्रति उन्हें पहुँचा दी और
अबकी बार नाटक शीघ्र ही पढ़ा भी गया। और कुछ ही अर्सा बाद
खेला भी गया और वह मकबूल भी हुआ और मेरी खुशी का ठिकाना नहीं
था कि स्क्रिप्ट के नाते प्रतियोगिता में पहले नंबर पर भी
आया।
नाटक अभी खेला ही जा रहा था
जब एक दिन प्रातः मुझे अमृता प्रीतम जी का टेलीफ़ोन आया।
मुझे नाटक पर मुबारकबाद देते हुए बोलीं,
''तुमने इमर्जेंसी पर खूब चोट की है। मुबारक हो!''
अमृता जी की ओर से मुबारक मिले इससे तो गहरा संतोष हुआ पर यह
कहना कि इमर्जेंसी पर मैंने चोट है, सुन कर मैं ज़रूर चौंका।
उन्हें इमर्जेंसी की क्या सूझी? इमर्जेंसी तो मेरे ख़्वाब
में भी नहीं थी। मैं तो वर्षों से अपनी ही इमर्जेंसी से
जूझता रहा था। बेशक ज़माना इमर्जेंसी का ही था जब नाटक ने
अंतिम रूप लिया। पर हाँ, इसमें संदेह नहीं कि निरंकुश
सत्ताधारियों के रहते, हर युग में, हर समाज में, हानूश जैसे
फ़नकारों के लिए इमर्जेंसी ही बनी रहती है, और वे अपनी निष्ठा
और आस्था के लिए यातनाएँ भोगते रहते हैं जैसे हानूश भोगता
रहा। यही उनकी नियति है।
१ अप्रैल २००७ |