|
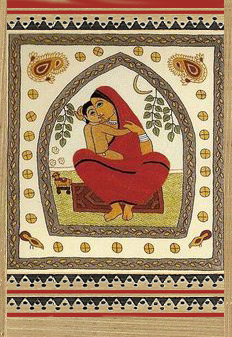
नवगीत परिसंवाद-२०१३ में
पढ़ा गया शोध-पत्र
गीत स्वीकृति: रचना प्रक्रिया के नए
तेवर
- वीरेन्द्र आस्तिक
गीत की स्वीकृति और उसकी रचना प्रक्रिया पर कुछ कहने
से पहले, यहाँ अपने एक पत्र को रखना चाहूँगा जो
'संचेतना' (दिल्ली: पूर्णांक-१५९) में छपा था। यह अंक
एक विशेषांक था- 'संकट गीत की स्वीकृति का।' पत्र का
मुख्यांश इस प्रकार था- "२० वीं सदी के उत्तरार्द्ध
में हिन्दी साहित्य में एक विस्मयकारी परिवर्तन देखने
में आया जिस पर आलोचकों का ध्यान या तो नहीं गया या वे
जानबूझकर, केन्द्रस्थ नहीं हुए। वह तथ्य था- कथ्यात्मक
स्तर पर हिन्दी की सारी विधाओं का एक होना, अर्थात्
विभिन्न विधाओं की आन्तरिक ध्वनि में एकात्मकता। यह एक
ऐसा तथ्य था जिस पर आलोचकों की कलम चलनी चाहिए थी,
किन्तु आश्चर्य, उक्त तथ्य की धवलता आलोचकीय कुहासे
में उभर नहीं पायी। विधाएँ अपने-अपने स्वरूप पर मुग्ध,
अपने-अपने शिविरीय आइनों में श्रेष्ठ साबित होती रहीं
और उक्त तथ्यात्मक वास्तविकता दबी रह गई। यह कथ्यात्मक
एकात्मकता यदि आलोचना के केन्द्र में आई होती तो कम से
कम काव्य जगत के विभिन्न स्वरूपों की समग्र रूप से
मूल्यांकन की धारा विकसित होती।"
विधाओं की संरचना में अन्तर होते हुए भी कथ्यात्मक
साम्य पर विचार किया जाए तो गीत की स्वीकृति अर्थात्
साहित्य की मुख्य धारा में उसकी भागीदारी का संकट,
निष्कर्षत, संकट नहीं रह जाता है। क्योंकि नवगीत के
रचनात्मक विकास के इतिहास को जब हम देखते हैं, तो पता
चलता है कि वहाँ गीत, समय की सापेक्षता, युगीन
सन्दर्भों और अपनी प्रभावोत्पादकता में ट्रैक से अलग
नहीं है। गीत और कविता के द्वन्द्वात्मक संबंधों के
बारे में यहाँ डॉ. वीरेन्द्र सिंह का कथन उद्धृत है-
'गीत और छन्दमुक्त कविता में यथार्थ को व्यक्त किया जा
सकता है। गीतों और कविताओं के अध्ययन से यह सत्य प्रकट
होता है कि गीतों में भी वही कहा जा सकता है जो
कविताओं में कहा जाता है। डॉ. सन्तोष कुमार तिवारी
जैसे आलोचक भी मानते हैं कि "जीवन मूल्यों की पहचान और
शब्द की गतिशील अर्थवत्ता की पकड़ दोनों विधाओं में
है।"
आलोचकों का उपरोक्त कथन अकारण नहीं है। वे कहना चाहते
हैं कि युग की परिवर्तनकामी प्रवृत्तियों से गीत-नवगीत
की रचना प्रक्रिया भी स्पर्धित हुई है। वहाँ भाषा में
नए मुहावरे गढ़े गए हैं तथा नवीन शब्द योजनाओं में समय
की त्रासदी और संवेदना व्यंजित हुई है। इस तरह यदि आज
के नवगीत की रचना प्रक्रिया के सन्दर्भ में कथ्यगत
विषयवस्तु, शैल्पिक भाषा और उसकी अन्विति
(प्रस्तुतीकरण) विधान आदि पर विचार कर लिया जाए तो गीत
के नए तेवरों का परिदृश्य सामने आ सकता है।
जहाँ तक कथ्य का प्रश्न है- मानता हूँ कि समकालीन
साहित्य में आम जनता के नायकत्व में मनुष्य के पूरे
जीवन दर्शन का केन्द्रस्थ होना ही कथ्यात्मक एकता की
सबसे बड़ी पहचान है। इसी से संलग्न दूसरी बात यह है कि
कथ्यात्मक एकता ही वह तथ्य है जिसके कारण हमारी
अनुभूतियों एवं विषय वस्तुओं में भी समानता व टकराहट
दिखाई देती है। क्योंकि मनुष्य ही साहित्य के केन्द्र
में है और वहाँ वह खानों में नहीं बँटा है। इन
तथ्यात्मक कसौटियों से रू-ब-रू गीत, साहित्य की विकास
यात्रा में अन्य विधाओं की तरह एक सहयात्री रहा है और
आज भी है।
दूसरी बात जो भाषा से संबद्ध है उस पर भी विचार कर
लेना चाहिए। क्योंकि रचना प्रक्रिया भी भाषा से ही
बनती है। सामान्यतः भाषा के निर्माण में 'मैटर और
मैनर' के संतुलन की कलात्मक भूमिका होती है। भाषा
स्वयं अपने ही घटकों कथ्याग्रहों, ऐन्द्रिय बिम्बों
एवं मुहावरों आदि के प्रयोग से प्रभावित होती है। भाषा
की कलात्मकता ही एक प्रकार के शिल्प का बोध कराती है।
किन्तु गीत की भाषा अन्य गद्य एवं गद्यात्मक विधाओं से
बिल्कुल भिन्न है। इस भिन्नता के मुख्य कारक हैं, छन्द
और प्रास, जो कविता के आलोचकों के समक्ष सबसे बड़ी
दुविधा एवं नकार के रूप में रहे हैं। उन लोगों का
मानना था कि जटिल अनुभूतियों वाले विषय गीत के लिये
उपयुक्त नहीं हो सकते या गीत ऐसे विषयों को काव्यत्व
प्रदान करने में अक्षम हैं। किन्तु समय के साथ गीत की
विकासात्मक प्रवृत्तियों ने इन सारे आरोपित फतवों का
उत्तर सहज अभिव्यक्ति के रूप में दिया है और आज भी दिए
जा रहा है।
उदाहरण के बतौर यहाँ डॉ. अवनीश सिंह चौहान का एक
गीत-'गली की धूल' पर बात की जा सकती है। समय और प्रगति
की द्वन्द्वात्मकता में हमारी जो अवनति हुई है-बताती
है कि हम भारतीय आधुनिक चिंतन के स्थापित मूल्यों से
कैसे और कितने ड्रैग हुए हैं। इस गीत की अर्थ-वीथियाँ
हमें कहाँ-कहाँ ले जाती हैं- उससे लगता है कि हमने
लक्ष्य के विपरीत दिशाओं में यात्राएँ की हैं-
समय की मार ही तो है। किया जिसने विखण्डित घर
गरीबी में जुड़े थे सब। तरक्की ने किया बेघर
किसी वाक्य की रचना में यदि छन्द-प्रास विद्यमान है तो
उसका कुल इतना ही मतलब है कि शब्दों को कुछ इस तरह
नियोजित कर दिया गया है जिससे उसका पाठ लयबद्ध अर्थात्
गेय हो गया है। गीत में लय-गेयता उसकी कलात्मकता का एक
पक्ष है जिससे गीत की विषयवस्तु आदि बिल्कुल भी आहत
नहीं होती। जैसा कि पारम्परिक छन्दों में प्रायः हो
जाया करता था। वहाँ मीटर प्रमुख था और कथ्य को गिराने
की छूट थी। नवगीत में कथ्य (यथार्थवादी रूझानों आदि के
कारण) प्रमुख हो गया। वहाँ कथ्य के अनुसार छन्दों का
निर्माण किया जाने लगा। गेय भाषा में विषयवस्तु की
बुनावट का कार्य कविता के किसी कवि के लिए जटिल हो
सकता है पर गीत साधक के लिए उसकी साधना की एक विशेष
नियति होती है जिसे लयप्रिय होना ही होता है। गीतकवि
छन्द-प्रास युक्त भाषा में वस्तु-प्राण वैसे ही
प्रतिष्ठित करता है जैसे कोई कवि या कथाकार गद्य में।
कहने का कुल आशय यह कि भाषा और वस्तु के
अन्योन्याश्रित संबंधों को गीतकार भी समझता है तथा
प्रयोग में भी लाता है। इस तरह अज्ञेय का कथन कि भाषा
कवि के प्रयोग का साधन है या काव्य के गुण अन्ततः
'भाषा के ही गुण होते हैं' का गीत पूरी तरह निर्वाह
करता है। ध्यातव्य है कि यह वक्तव्य अज्ञेय ने कविता
के पक्ष में दिया था।
उपरोक्त विवेचन के बाद एक पक्ष और रह जाता है गीत की
अन्विति अर्थात वस्तु और भाषा के अन्योयाश्रित संबंध
के आधार पर अर्थात्मक पूर्णता का। कविता की
आलोचना-भाषा में अन्विति को 'अर्थ की लय' कहा गया है।
जबकि गीत में अर्थ की लय गम्भीर से गम्भीर हो जाने की
प्रक्रिया में गतिमान रहती है। गीत प्रायः अपनी अन्तिम
पंक्तियों में सर्वाधिक पोटेंशियल होता है। कविता की
पोटेंसी के संदर्भ में यहाँ पर रामस्वरूप चतुर्वेदी का
कथन प्रासंगिक है- "कविता उत्कृष्टतम शब्दों का
उत्कृष्टतम क्रम है।" स्थूल रूप से यह परिभाषा गीत के
लिए अपर्याप्त-सी जान पड़ती है। उत्कृष्टतम शब्दों को
उत्कृष्टतम क्रम में रखना ही कलात्मकता है। 'क्रम'
शब्द से विन्यास जैसा भाव भी ध्वनित होता है जो अन्ततः
छन्द की ओर संकेत करता है। दरअसल वे कहना चाहते होंगे
कि "कविता (गीत भी) श्रेष्ठतम भाव के लिए उत्कृष्टतम
शब्दों का उत्कृष्टतम कलात्मक रूप है।"
प्रसंगत अवगत हो कि आलोचकों में 'रूप' शब्द विवाद का
विषय रहा है। वे कविता को रूप से बाहर रखते रहे हैं और
गीत के रूप से 'एलर्जी' (वही छन्दादि के कारण)। मैं
कहना चाहता हूँ कि वस्तु और रूप का संबंध तो आत्मा और
शरीर जैसा होता है। माना कि सर्जना की श्रेष्ठता
वस्तु-तत्व पर निर्भर करती है, किन्तु शैल्पिक शरीर
वस्तुतः कथ्यवस्तु पर स्वयं की आन्तरिक माँग के अनुसार
ही तो उत्सर्जित होता है। जैसा डॉ.सन्तोष कुमार तिवारी
कहते हैं कि "तत्व के भीतर से ही रूप स्वयं ढलने लगता
है।" अर्थात चाहे कितना ही अमूर्त्त काव्य क्यों न हो
वह शब्दों में अवतरित होते ही मूर्त्तमान हो जाता है।
रूप है तो, किसी न किसी प्रकार की लय अवश्य उत्पन्न
होगी और दोनों के संयोग से सौंदर्य की भाषा, भी बोध
में आएगी। उक्त तथ्यों के आधार पर कविता भी छान्दसिक
आवश्यकताओं से इन्कार नहीं कर सकती। कविता की भाषा
विशुद्ध गद्य नहीं है। कविता की रचना प्रक्रिया में भी
काव्य आधारित कोई न कोई लय निर्माण की प्रक्रिया चलती
रहती है। गीत हो या कविता दोनों में लय का सर्वाधिक
महत्व स्वीकार किया गया है लय का प्रबन्ध ही तो छन्द
है अतः कविता में भी छन्द का अस्तित्व न्यूनाधिक रूप
में विद्यमान रहता है।
यहाँ गीत और कविता के बारे में उपरोक्त तथ्यों को
प्रस्तुत करने का कुल आशय यही रहा कि उनमें रचनात्मक
स्तर पर तो अन्तर रहेगा किन्तु अर्थात्मक और भावबोध के
स्तर पर दोनों विधाएँ युग सापेक्ष तथा समकालीन हैं। इस
आधार पर केवल गीत को मूल्यांकन व मुख्यधारा के दायरे
से बाहर रखना दुखद तो है ही, एक षडयंत्र भी है।
गीत स्वीकृति: रचना प्रक्रिया के नए तेवर (भाग-२)
सन् १९६० के बाद गीतों में कथ्य की माँग के अनुसार
छन्दों का प्रयोग करने का चलन बढ़ता गया। इनमें
पारम्परिक छन्दों के भी प्रयोग होते रहे, किन्तु
अधिकतर उनकी लयों के लघु आकार (लंबाई) ही अपनाए गए।
संक्षिप्त कथ्य वस्तु या अर्थ संप्रेषण आदि की वजह से।
यहाँ पर पहले 'कथ्य की माँग' और अनुभूति के
अंतर्सम्बन्धों को समझना जरूरी होगा। इम देखते हैं कि
साहित्यिक धाराओं में आम जनता का व्यवस्था आदि के
प्रति बढ़ता आक्रोश और नैराश्य आदि एक महत्वपूर्ण
भूमिका प्रस्तुत करता गया है। इस आक्रोश का कारण भले
ही राजनीतिक रहा हो, किन्तु इस सच्चाई से इन्कार करना
बेमानी होगा कि इसी काल में चीन और पाक युद्धों का
सामना करना पड़ा। वास्तव में यह काल हमारे लिए किसी
वज्रपात को झेलकर सँभलने का काल था।
अगले दशकों में आशातीत आश्वासनों और निष्ठाओं पर बेबाक
एवं मारक अभिव्यक्ति का प्रहार होना जो प्रारम्भ हुआ
तो उससे अनुभूति का आधार एकाएक परिवर्तित होते देखा
गया अर्थात् वहाँ युग यथार्थ और उसकी मूल संवेदना ही
आत्मानुभूति का रूप ग्रहण करती गई है। आलोचक इसी
प्रक्रिया को रचना में अनुभूति जन्य वैचारिकता या
विचारजन्य अनुभूति का आधार बनना देखते हैं। यहाँ पर
तेजी से बदलते अनुभूति के आधारों और उसके सौंदर्य को
आत्मसात करना होगा, तभी हम गीत की नई अंतर्वस्तु और
उसकी रचना प्रक्रिया के साथ न्याय कर सकेंगे। इस काल
में नित्य बदलते घटनाक्रम के सामाजिक बीहड़ में अनुभूति
के छोटे-छोटे अंशों को गीत में 'फोकस' करने का प्रचलन
अधिक बढ़ा जिससे गीत अधिकाधिक पोटेंशियल हुआ। डॉ.
रवीन्द्र प्रभार, वीरेन्द्र मिश्र, नईम, शिव बहादुर
सिंह भदौरिया, देवेन्द्र शर्मा इन्द्र, सत्य नारायण,
शांति सुमन, विद्या नंदन, राजीव, माहेश्वर तिवारी आदि
के गीत उपरोक्त तथ्यों के आधार पर परखे जा सकते हैं।
इस काल के नवगीतों में समाजिक, आर्थिक मूल्यों के अलावा
व्यक्तित्व बोध और भारतीय जीवन दर्शन का अद्भुत
सामंजस्य हुआ है। इस पीढ़ी का उत्तर काल जो हमें विरासत
में मिला है वह कम महत्वपूर्ण नहीं, इस धारा का
आगे विकास होना चाहिए। शिव बहादुर भदौरिया का एक नवगीत
उपरोक्त आशय का मार्मिक बोध कराने में बेजोड़ है-
मेरी कोशिश है कि
नदी का बहना मुझमें हो
मैं न रूकूँ संग्रह के घर में
धार रहे मेरे तेवर में
मेरा बदन काट कर नहरें
ले जाएँ पानी ऊसर में
जहाँ कहीं हो बंजरपन, का
मरना मुझमें हो
पूरा गीत विश्वबंधुत्व, उसकी सार्वभौमिक दृष्टि और
उदारवादी नीति का बोध कराता है। नवगीत वैश्विक मूल्यों
और भारतीय आधुनिक सांस्कृतिक मूल्यों में सामंजस्य
स्थापित करने का सफल प्रयास करता आया है, मूल्याकंन की
दृष्टि से यह भी देखा जा सकता है बल्कि देखा जाना
चाहिए कि रचना अपनी सोद्देश्यता के संप्रेषण में कितनी
अर्थवान है। पुरानी पीढ़ी के बाद विशेषतः दशकीय
प्रवृत्तियों के नवगीतों से जो नवगीत परिभाषित हुआ,
उसका प्रभाव बाद की नई पीढ़ी में भी देखा जा सकता है-
अजय पाठक, यश मालवीय, मनोज जैन मधुर, अवनीश सिंह
चौहान, यशोधरा राठौर आदि के गीतों में युगीन
पारदर्शिता स्पष्ट हुई है। ऐसे गीत भूमण्डलीय विभीषिका
(बाजार सभ्यता) और भारतीय चिंतन की द्वन्द्वात्मकता
में दरअसल उन भारतीय मूल्यों को सुरक्षित रखना चाहते
हैं, जिन मूल्यों को विश्व बिरादरी ने सम्मानजनक
दृष्टि से देखा है। ऐसे तथ्यों के सन्दर्भ में मनोज
जैन मधुर का कहना है-
इच्छाओं की फौज बिदकती/ जब-जब भटका मन
थमा दिया दुख के हाथों ने/ जीवन का दर्शन
विश्वग्राम से लोक ग्राम की/ देह रही है छिल
आखर कबिरा की साखी के/ दिखते हैं धूमिल
तम्बू तने हुए ज्यों के त्यों/ नई-पुरानी रीत के
(एक बूँद हम: पृष्ठः ५४-५५)
कहना होगा कि गीत आनुभूतिक प्रखरता/प्रधानता के कारण
ही संक्षिप्त हुआ और इसी से जुड़ते रचना प्रक्रिया के
अन्य घटक भी प्रभावित हुए। पहले से टेक आवृत्ति भी
तार्किक हुई। शब्द औचित्य चिंतन द्वारा निरर्थक या
साधारण से शब्दों से किनाराकशी तथा तुकांत इतने
अर्थप्रिय प्रयोग में लाए जाने लगे जो पंक्ति में
ठुँसे न होकर आवश्यक प्रतीत हों।
दरअसल गीत समय का दस्तावेज बनने की जद्दोजहद में
प्रयोग धर्मी होता गया है। वास्तव में गीत का
प्रयोगधर्मी होना ही नवीन होना है। प्रयोग किसी एक अंग
पर केन्द्रित नहीं होता, वह रचना प्रक्रिया को अपनी
सर्वांगिकता में देखता है। हम कह सकते हैं कि कथ्य,
छन्द और प्रास आदि के संगुफित प्रयोगों से आनुभूतिक
प्रभावोत्पादन की अनूठी खोज हुई है। कहना चाहूँगा कि
प्रयोग प्रक्रिया भाषा की वह रेसिपी है जिसमें रचनाकार
अपने अनुभूत तत्व को घुलते हुए देखता है तथा संवेदना
और उत्पीड़न आदि के द्वन्द्वात्मक मूल्य को निथरते हुए
भी देखता है। डॉ. विष्णु विराट की गहन प्रक्रिया से
उक्त तथ्य स्पष्ट होता है-
जुर्म ये है कि जुर्म कुछ भी नहीं
फिर भी गर्दन तो कटारी पर है
ठोकरें उनको कहाँ छू पातीं
वे तो घोड़े की सवारी पर हैं।
एक बात और छन्द की सहजता पर। आचार्य महावीर प्रसाद
द्विवेदी ने कभी कहा होगा कि गद्य और पद्य की भाषा
पृथक-पृथक नहीं होनी चाहिए। 'भाषा' का अर्थ यहाँ पद्य
का गद्य में रूपान्तरित होना नहीं, बल्कि भावार्थ की
दृष्टि से पद्य की स्पष्ट रचना प्रक्रिया से है। दरअसल
क्लिष्टात्मक शिल्प जितना सहज होता जाता है लयात्मकता
उतनी ही गद्यात्मकता का आभास देती है। सत्य नारायण की
गीत पुस्तक की भूमिका में कन्हैयालाल नंदन ने एक गीत
को गद्य के रूप में लिखकर उक्त कथन की पुष्टि की, जबकि
गीत अपने छन्द विधान में पूर्ण है। गीत है- "सभाध्यक्ष
हँस रहा, सभासद कोरस गाते हैं। जय-जयकारों का अनहद है,
जलते जंगल में, कौन विलाप सुनेगा घर का, इस कोलाहल
में......आप चक्रवर्ती हैं राजन, वे चिल्लाते हैं।"
यहाँ पर बनन-कहन भंगिमा नए प्रतिमानों का सहारा लेकर
सहज किन्तु नए अन्वेषण के रूप में प्रगट हुई है।
गीत-भाषा में संवाद तत्व और नामों के प्रयोग भी सार्थक
हुए हैं, जो प्रायः प्रतीक के रूप में अपनाए जाते हैं।
ऐसे शब्द ऐतिहासिक/वैज्ञानिक और राजनैतिक घटनाओं आदि
को अपने में समेटे हुए मिथकीय रूप में भी आते हैं।
हिन्दी कविता में प्रतीक (मिथक) रूप में कबीर शब्द का
प्रयोग बहुतायत है। अवध बिहारी श्रीवास्तव का एक गीत
है-मंडी चले कबीर। कबीर शब्द अनेक ध्वन्यार्थों में
प्रयुक्त होता रहा है। यहाँ गीत में वह एक आम आदमी है
जिसका शोषण हो रहा है।
अर्थात् शोषक-शोषित संबंधों की अभिव्यक्ति में उक्त
प्रकार का प्रयोग हुआ है-"कपड़ा बुनकर/थैला लेकर/मंडी
चले कबीर/जोड़ रहे हैं रस्ते भर वे/लगे सूत का
दाम/ताना-बाना और बुनाई, बीच कहाँ विश्राम/कम से कम
इतनी लागत तो पाने हेतु अधीर/कोई नहीं तिजोरी खोले,
होती जाती शाम/उन्हें पता है कब बेचेंगे औने-पौने
दाम/रोटी और नमक थैलों को, बाजारों को खीर।"
उपर्युक्त कुल विवेचन का सरांश यही है कि हिन्दी
आलोचना में गीत की स्वीकृति का संकट, संकट नहीं बल्कि
गीत को हाशिए पर रखने का षड़यंत्र मात्र है जो यहाँ
शब्दशः स्पष्ट हुआ है जिन आलोचकों को छन्द-प्रास से
एलर्जी है उन्हें अब अपना दृष्टिकोण बदलना होगा। बात
बिल्कुल साफ हे कि छन्द-प्रास गीत की कलात्मकता के
अनिवार्य अंग हैं तथा इनकी वजह से विषय वस्तु की
गम्भीरता आहत न होकर अधिकाधिक संप्रेष्य हो जाती है।
उन आलोचकों को भी अपने निष्कर्ष बदलने होंगे जिनके
विचार थे कि जटिल अनुभूतियों वाले विषय गीत के लिए
उपयुक्त नहीं हो सकते। वास्तविकता ये है कि युगीन
परिवर्तनों के कारण गीत में भी वैचारिक एवं आनुभूतिक
स्तर पर परिवर्तन आते हैं जिनका वह नए-नए
भाषा-प्रयोगों द्वारा अपने में समाहार करता है। आज
संरचनात्मक भेद होते हुए भी गीत और कविता में
कथ्यात्मक स्तर पर समानता देखी जा सकती है। सिक्के का
दूसरा पहलू यह भी है कि भारत एक गीत प्रधान देश है
जहाँ गीत की स्वीकृति का मुद्दा ही बेबुनियाद है।
हकीकत यह भी है कि साहित्य समाज में गीत के स्वीकार
भाव को हमेशा आदर मिला है वहीं गद्य कविता की
प्रासंगिकता पर प्रश्नचिन्ह लगते रहे हैं। आज गीत की
नवांतर रचना प्रक्रिया ने यह सिद्ध करके दिखला दिया है
कि गीत एक युगानुरूप प्रगतिशील काव्य प्रवाह है। |