|
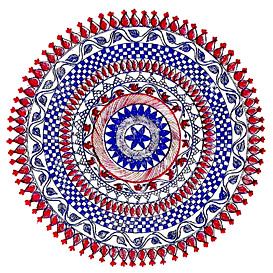
नवगीत परिसंवाद-२०१३ में
पढ़ा गया शोध-पत्र
समकालीन गीतों में
संवेदना के विकास का स्वरूप
-
नचिकेता
लिरिसिज्म की वैयक्तिकता
का एक स्तर ऐसा अवश्य है जो आज भी हमें उससे जोड़ देता
हैः शायद आदिम मानव की भावनाएँ हमारे भीतर अब भी
विरासत के रूप में उपलब्ध हैं। लिरिसिज्म सनातन है,
अर्थात यदि इसे हम साहित्य के विकास की प्रथम
पूर्णावस्था मानें तो वह इस ड्रामेटिक काल की
पूर्णावस्था में भी विद्यमान है।...वरन् आज का
लिरिसिज्म एक जटिल, मर्माहत, कुंठित संवेदना का उपादान
है जो जीवन और सत्य के प्रोजयिक पक्ष को उभारता है और
यही कारण है, आज का लिरिसिज्म हमें तिलमिला देता है,
उसमें एक पैथस है जो मूलतः वैयक्तिक होते हुए भी
प्रोजयिक पक्ष की कलेक्टिव रियलिटी के भाव-बोध को
लिये है, उससे संघटित है। गीत और गीतात्मकताके संदर्भ
में नयी कविता, खासकर साठोत्तरी कविता, के एक अत्यंत
ही महत्त्वपूर्ण कवि-विचारक मलयज की इस टिप्पणी में
गीत-रचना की रचनात्मकता, उसमें अंतर्निहित आत्मपरकता,
समसामयिकता और सामाजिकता पर पुनर्विचार करने के कई
सूत्र मौजूद हैं। वैसे गीत के सवाल पर हिंदी आलोचना
काफी उलझी हुई दृष्टिगत होती है।
‘हिंदी साहित्य-कोश,
भाग-१’ के अनुसार कवि की वैयक्तिक भावधरा और अनुभूति
को उसके अनुरूप लयात्मक अभिव्यक्ति देने के विधान को
‘गीतिकाव्य’ कहते हैं तथा गेयता, भाव-प्रवणता,
आत्माभिव्यक्ति, रागात्मक अन्विति, कोमलकांत पदावली,
सौंदर्यमयी कल्पना आदि गीतिकाव्य के मूल तत्त्व हैं, हिंदी आलोचना की पारिभाषिक शब्दावली। गीत को
वैयक्तिक, आत्मपरक, अत्यंत सघन और कोमल अनुभूतिजन्य
रचना मानने में मार्क्स वादी आलोचक भी पीछे दिखाई नहीं
देते। नामवर सिंह की दृष्टि में गीत निजी आत्मानुभूति
की अभिव्यक्ति का माध्यम है। जबकि उन्हें यह तो मालूम
होगा कि गीत आदिम वर्गविहीन समाज में सामूहिक
श्रम-प्रक्रिया के दौरान आदिम मनुष्यों की माँसपेशियों
में आने वाले तनाव के संकोच और विस्तार तथा संवेग के
आरोह-अवरोह से उत्पन्न लय ने ही उस काल के मनुष्यों के
श्रम-परिहार के लिए समूहगीत का आकार ग्रहण किया था। तब
श्रम का विभाजन, निजी पूँजी एवं समाज में वर्ग-विभाजन
का आरंभ नहीं हुआ था। जाहिर है कि तब सामूहिक संवेग की
ही उत्पत्ति संभव थी, जिसकी अभिव्यक्ति तत्कालीन
समूहगीतों में हुई थी। सामूहिक संवेग के गर्भ से
उत्पन्न गीत को निजी आत्मानुभूति का माध्यम मानना कहाँ
से उचित माना जा सकता है?
दरअसल गीत आत्मपरक, संगीतात्मक और रागात्मक रचना होता
है, किंतु गीत की आत्मपरकता में अंतर्निहित मानवीयता
की आवाज सुनकर ही गीत के मर्म तक पहुँचा जा सकता है।
यह बात दीगर है कि गीत-रचना में सामाजिक
अनुभव को भी वैयक्तिक अनुभव के साँचे में ढालकर अत्यंत
ही सघन रूप में व्यक्त किया जाता है। अतः गीत जटिल
जीवन और सत्य के प्रोजयिक पक्ष को ही नहीं, वरन् उसके
संगीतात्मक पक्ष को भी अत्यंत ही सार-रूप में प्रस्तुत
करता
है। इसीलिए यह आज के ड्रामेटिक काल में भी कलेक्टिव
रियलिटी संश्लिष्ट यथार्थद्ध के संघटित भावबोध को
अभिव्यक्त करने में सफल होता है।
गीत की आत्मपरकता को
व्यक्तिनिष्ठता का पर्याय मानने में गीतकार आलोचकों से
तनिक भी पीछे नहीं हैं। वर्ष १९७१ में प्रकाशित अपने
गीत-संग्रह ‘ओ प्रतीक्षित’ को हिंदी की एक प्रख्यात
गीत-कवयित्री ने ‘पति को, साथ जिये गीतिल क्षणों के
लिए’ समर्पित किया है। यह साधारण अभिकथन नहीं है।
दरहकीकत यह समर्पण संपूर्ण ‘पति को’ नहीं, प्रत्युत
पति के साथ जिये हुए चरम सुख के नितांत निजी और घनीभूत
क्षणों को समर्पित है, जिसकी सहजानुभूति हर मनुष्य को
नहीं हो सकती। यही निजी आत्मानुभूति का बीज मंत्र है,
क्योंकि उस घनीभूत और नितांत निजी अनुभूति को ‘गीतिल’
विशेषण से नवाजा गया है यानी गीतकर्त्री भी मानती है
कि गीत नितांत निजी आत्मानुभूति का माध्यम है। हालाँकि
‘ओ प्रतीक्षित’ को नवगीत-संग्रह कहा गया है। जबकि यह
ऐतिहासिक सत्य है कि नवगीत ने गीत को वैयक्तिक और
आत्मनिष्ठ आत्मानुभूति के दायरे से बाहर निकाल कर
यथार्थवादी और वस्तुपरक अनुभूति की अभिव्यक्ति का
माध्यम बनाया है। अपने समय के तमाम सामाजिक यथार्थ,
उसके अंतर्विरोधों, आर्थिक विषमताओं, राजनीतिक
विसंगतियों और विद्रूपताओं तथा सांस्कृतिक विडंबनाओं
को अनुभूतिपरक अभिव्यक्ति के रूप में ढाल दिया है।
जिससे उसकी वस्तुगत दुनिया और संवेदना का फलक काफी
चौड़ा एवं उर्वर हो गया है। दुर्भाग्य है कि नवगीत पर
विचार करने के समय हम प्रायः इस अनावश्यक बहस में उलझ
जाते हैं कि नवगीत शब्द के प्रथम प्रयोक्ता राजेंद्र
प्रसाद सिंह हैं या शंभूनाथ सिंह या कोई अन्य। हम यह
जानने की चेष्टा तक नहीं करते कि नवगीत के उदय के लगभग
साठ वर्ष गुजर जाने के बाद नवगीत की संवेदना के विकास
का स्वरूप या गति क्या और कैसी रही है। ध्यातव्य है कि
साहित्य में संवेदना का विकास अनायास, अप्रत्याशित,
स्वतःस्फूर्त और आसमानी ढंग से नहीं होता, अपितु इसकी
जड़ें सामाजिक विकास की ऐतिहासिक और प्रगतिशील परंपराओं
का खाद-पानी पाकर गहरे गड़ती और पसरती हैं आगे फूलती और
फलती हैं।
‘मेरे गीत और कला’
शीर्षक आलेख में निराला ने आगाह किया है कि मेरी ऐसी
रचना नहीं, कि सूक्ति-रूप में इसका एक अंश उद्धृत किया
जा सके। मेरी छोटी रचनाएँ (लिरिक्स) और गीत (सांग्स)
प्रायः ऐसी ही हैं। इसकी कला इसके संपूर्ण रूप में है,
खण्ड रूप में नहीं। वास्तव में, गीत के मूल्यांकन में
उसका कोई एक अंश सूक्ति-रूप में उद्धृत करना लाजमी
नहीं होता, क्योंकि गीत की बनावट और बुनावट इतनी गझिन
और संक्षिप्त होती है कि उसके एक अंश मात्रा के जरिए
उसके पूरे अर्थ-बोध और कलात्मक सौंदर्य का मुकम्मल
उद्घाटन संभव नहीं है। इसलिए हम अपने पाठ में हर
रचनाकार के पूर्ण गीत के साथ अनुक्रिया करेंगे, अंश
रूप में नहीं। निराला का प्रसिद्ध गीत है, जिसकी रचना
१९५१ में हुई है-बाँधे न नाव इस ठाँव, बंधु/ पूछेगा
सारा गाँव, बंधु/ यह घाट वही जिस पर हँसकर/ वह कभी
नहाती थी घँसकर/ आँखें रह जाती थीं फँसकर/ कँपते थे
दोनों पाँव, बंधु/ बाँधे न नाव इस ठाँव, बंधु/ वह हँसी
बहुत कुछ कहती थी/ सबकी सुनती थी, सहती थी/ फिर भी
अपने में रहती थी/ देती थी सबको दाँव, बंधु/ बाँधे न
नाव इस ठाँव, बंधु।
आकारगत संक्षिप्तता, रूप-सौष्ठव,
आंतरिक संघटन, भाव-संहति और संगीतात्मक अंविति के
हिसाब से निराला का यह गीत निस्संदेह अन्यतम है। इस
गीत में दो बंद और कुल दस पंक्तियाँ हैं। इसकी सभी
पंक्तियाँ समचरणांत यानी सोलह मात्रावाले छंद में
निबद्ध हैं। इसके टेक की सभी पंक्तियाँ भी समान
ध्वनिवाली हैं। इनमें क्षीप्र गतिशीलता है। पूरे गीत
का भाव एक प्रश्नाकुल जिज्ञासा से आवेष्ठित है और जो
गीत के अंत तक बरकरार रहता है।
यह किसी भी उत्तम
गीत-रचना को अत्यंत ही प्रभावशाली बनानेवाला कारक है।
लेकिन इस गीत के केंद्रीय भाव में
उत्तरछायावादी दौर के
आत्मनिष्ठ प्रेम के दुख, दर्द और वियोग की वेदना और
मिलनोच्छवास की भावना ही अभिव्यक्त हुई है।
इस गीत का केंद्रीय भाव, वस्तुत: एक लोकगीत पर आधरित
है तथा इस गीत में लोकगीत की लय और धुनों का कलात्मक
समाहार है। काव्यभाषा भी लोकगीत जितनी ही सहज है। इसमें
तत्सम शब्दों के बनिस्पत देशज शब्दों के प्रयोग पर
अधिक भरोसा किया गया है। जो आधुनिक गीत के विकास के
अगले सोपान का द्योतक है।
निराला के इस गीत की
वैचारिक अंतर्वस्तु रूप में एक युवा जोड़े,
स्त्री-पुरुष का नैसर्गिक प्रेम ही
अवस्थित
है, जो अंत-अंत तक अव्यक्त ही रहता है। स्त्री-पुरुष
दोनों एक-दूसरे से उद्दाम प्रेम करते हैं, दोनों को इस
बात की
जानकारी और अहसास है, फिर भी उनका प्रेम अव्यक्त रह
जाता है, अर्थात दोनों एक-दूसरे से वस्तुवादी प्रेम नहीं
करते,
अपितु, 'प्लोटोनिक लव करते हैं। निराला से दशकों पूर्व
चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने अपनी प्रसिद्ध कहानी 'उसने कहा
था
में इस आत्मनिष्ठ, किंतु अव्यक्त प्रेम को अत्यंत ही
मार्मिक अभिव्यक्ति देने की पहल की है, जिसमें उन्हें
अपूर्व
सफलता भी मिली है। गुलेरी का नायक भी अपने आत्मनिष्ठ
प्रेम को अपनी प्रेमिका के आगे कभी खुले रूप में व्यक्त
नहीं करता, परंतु उसके आत्मीय आग्रह का मान रखने की
खातिर अपने प्राण तक का उत्सर्ग कर देता है, वहीं
निराला
के गीत की नायिका अपने प्रेमी को अंत-अंत तक 'दाँव ही
देती रही है।
आधुनिकताबोध के धरातल पर निराला का
यह गीत आधुनिक जरूर है, किंतु 'उसने कहा था का
आदर्शवाद इस आधुनिकता से अधिक विश्वसनीय और प्रभावशाली तथा भारतीय जन-मानस के अधिक करीब दिखार्इ देता
है। पाँचवें दशक के अंत में भारत आजाद हो चुका था
और छठे दशक के आरंभ से ही भारतीय समाज के आधुनिकीकरण
की प्रक्रिया तेज हो चुकी थी। नतीजतन निराला
के इस गीत की संवेदना को हम विकसित दौर की संवेदना नहीं
मान सकते, बल्कि इस गीत को पिछड़ी संवेदना की रचना माने
तो कोर्इ अत्युकित नहीं होगी, क्योंकि छठे दशक के
भारतीय समाज में प्रेम-विषयक जड़ता अगर निर्मूल
नहीं
हुर्इ थी तो शिथिल जरूर हो गयी थी। प्रेम परवान चढ़े
या न चढ़े, मगर उसके इजहार की प्रवृत्ति तो वैदिक काल
में
भी विद्यमान थी, अन्यथा ऋग्वेद में लोपामुद्रा पुरुषों
को वशीभूत करने वाले मंत्रों का निर्माण करने में
सफल नहीं होती।
छठे दशक में ही लिखे गये केदारनाथ अग्रवाल के गीत की
संवेदना निराला के इस गीत की संवेदना से
अधिक विकसित और प्रगतिशील दृष्टिगोचर होती है। केदार का
गीत इस प्रकार है- माँझी, न बजाओ वंशी
/ मेरा मन
डोलता / मेरा मन डोलता जैसे जल डोलता
/ जल का जहाज जैसे
पल-पल डोलता / माँझी, न बजाओ वंशी
/ मेरा मन
डोलता / माँझी, न बजाओ वंशी
/ मेरा प्रन टूटता मेरा प्रन
टूटता/ है जैसे तृन टूटता
/ तन का निवास जैसे बन-बन टूटता/
माँझी, न बजाओ वंशी /
मेरा प्रन टूटता / माँझी, न बजाओ वंशी
/ मेरा तन झूमता मेरा तन झूमता
/ तेरा तन झूमता /
मेरा तन, तेरा तन, एक बन झूमता
/ माँझी, न बजाओ वंशी मेरा
तन झूमता।
केदारनाथ अग्रवाल का यह गीत भी निराला के गीत की भाँति
लोकगीत के साँचे और कहन शैली में
बँध एक प्रयोगधर्मी गीत है। इसकी सभी पंक्तियाँ
समचरणांत नहीं हैं, सभी पंक्तियों की मात्राएँ भी समान
नहीं हैं अर्थात
एक तारतम्य में बँधी विषम लय का इनमें एक लचीलापन
दृष्टिगत होता है और न ही टेक की सभी पंक्तियों में समान
ध्वनिवाले शब्दों का अनुधवन है, बल्कि इसके तीन बंदों
में तीन अलग-अलग टेकों का प्रयोग है, केवल तीनों बंदों
की लयानिवति समान है, जिससे तीनों बंद एक ही गीत के
अंग बन जाते हैं।
यह गीत, दरअसल टेक, तुक और समान
पंक्तियों वाली लय से परिचालित न होकर लोकगीत की तरह एक
लचीली लय से परिचालित है। केदार के गीत के
तीनों बंदों के आरंभ में लोकगीत की भाँति ही पहली
अर्धाली की आवृत्ति होती है और इस गीत का केंद्रीय भाव
भी
स्वकीया प्रेमोल्लास है। स्वकीया प्रेमोल्लास की
पराकाष्ठा है यहाँ। इसमें दो तन आपस में मिलकर एक हो
जाते हैं और
प्रेम के एकात्म अद्वैत की रचना करते हैं। यह आधुनिक
गीत-रचना का एक नया गवाक्ष है। इस गीत के प्रमोल्लास
की
अभिव्यक्ति में कृष्ण और राधा के मिथकीय प्रेम की
प्रतिध्वनि सुनार्इ देती है। प्रेमोल्लास का यह एकात्म
अद्वैत मेरी
जानकारी में सिर्फ भक्तकवि सूरदास के यहाँ है।
"अरुझी
कुंडल लट/ बेसरि सौं पीत पट/ बनमाल बीच आनि उरझें
हैं दोउफजन प्राननि सौं प्राण/ नैन नैननि अँटकि रहे/
चटकीली छवि देख लपटात श्याम घन होड़ा होड़ी नृत्य
करैं/ रीझि-रीझि अंक भरैं/ ता-ता-थेर्इ-थेर्इ उछटत है हरखि
मन सूरदास प्रभु प्यारी/ मंडली जुबति भारी/ नारी कौ
आँचल लै-लै पोंछत है श्रम कन"। स्पष्ट है कि निराला के इस
गीत की तुलना में केदारनाथ अग्रवाल का गीत अधिक प्रयोगधर्मी, आधुनिक और प्रगतिशील है तथा केदार के इस गीत
की संवेदना निराला के पूर्वोक्त गीत की संवेदना से
अधिक विकसित, युगसापेक्ष और समयसापेक्ष है।
गीत की संवेदना के विकास का अगला चरण हमें सातवें दशक
में लिखे शलभ श्रीराम सिंह के इस गीत
में दिखार्इ देता है- "शंख फूँका साँझ का तुम ने
/ जलाया
आरती का दीप / आँचल को उठाकर
/ बहुत धीमे
/ और धीमे
/ माथ से अपने लगाकर/
सुगबुगाते होंठ से इतना कहा-/
हे
साँझ मइया...। और इतने में कहा माँ ने-
/ बड़का आ गया/
बहन बोली: आ गए भइया/
और तुम ने/ गहगहार्इ साँझ में
/ फूले
हुए मन को सँभाले / हाथ जोड़े
फिर कहा.../ हे...साँ...झ...मइ...या।" इस गीत की संवेदना
और रचना-विधान दोनों अलग से विचार-विमर्श की माँग करते
प्रतीत
होते हैं। इस गीत में मध्यवर्गीय भारतीय गृहस्थ-वधू की
नितांत निजी संवेदना को बेहद संवेदनशील अभिव्यक्ति मिली
है, जिसका पति बाहर नौकरी करता है और काफी दिनों से
घर नहीं आया है। इस गीत में व्यक्त उस गृहस्थ-वधू की
नितांत निजी आत्मानुभूति निरा वैयक्तिक होते हुए भी
सामाजिक आत्मानुभूति का प्रतिनिधित्व करती है। इस गीत
के
एक-एक शब्द, एक-एक अक्षर बिलकुल नपे-तुले और अर्थपूर्ण
हैं। यह गीत गीत-रचना के पारंपरिक ढाँचे का
कलात्मक प्रतिरोध करता है और अपनी व्यापक काव्यात्मकता
की बदौलत अपने पाठकों की संवेदना से एकरूप हो जाता
है। गीत की गेयता पाठ में रूपांतरित हो जाती है अर्थात
गीत यहाँ श्रव्य काव्य न होकर पठ्य काव्य में परिवर्तित
हो जाता
है। पारंपरिक गीत से नवगीत की यह भिन्नता अलग से
द्रष्टव्य है। इस गीत की नायिका मुखर रूप से कुछ कहती
नहीं
है, किंतु गीत का हर शब्द उसकी विरह वेदना, मिलन की
कामना, सामाजिक आचार-व्यवहार, साँझ मइया से पति की
वापसी के निमित की गर्इ प्रार्थना और पति के आगमन की
सूचना पाकर साँझ मइया के प्रति हार्दिक आभार तथा उसकी
अनिर्वचनीय खुशी का इजहार करते दृष्टिगोचर होते हैं। एक
अच्छे गीत की यही पहचान भी है कि उसमें कम-से-कम
शब्दों में सामाजिक यथार्थ की उसकी संपूर्ण जटिलता के
साथ समग्रता में अभिव्यक्त हो।
ऐसी बात नहीं है कि केवल स्त्रियाँ ही अपने पति के
वियोग की घनीभूत वेदना से दग्ध होती हैं, पुरुष भी
अपनी प्रिया के वियोग में उतना ही तड़पता है। उत्तर
छायावादी दौर की लगभग सारी गीत-रचनाएँ इस विरह वेदना
की
गलदश्रु भावुकता की गिरफ्त में रही हैं। यह अलग बात है
कि उत्तरछायावादी दौर की विरह वेदना वायवी, काल्पनिक
और परकीया प्रेम की असामाजिक विरह वेदना है, इसमें
अतृप्त यौनेच्छा और मानसिक कुण्ठा का इजहार अधिक हुआ
है। इसके ठीक विपरीत नवगीत की विरह वेदना वास्तविक,
स्वाभाविक और सामाजिक, स्वकीया प्रेम की विरह वेदना
है, इसलिए इसमें अनावश्यक भाव-स्फीति, कल्पना की ऊँची-ऊँची उड़ानें, नाजुकखयाली और खूबसूरत अंदाजेबयाँ
नहीं
है। इसकी जगह यहाँ जीवन-संघर्ष की तपिश और वास्तविक
जीवन-यथार्थ की जटिलताएँ अधिक चित्रित हुर्इ हैं। इसमें
दैनंदिन जीवन के सामान्य क्रियाकलापों के बीच अपनी
प्रिया, पत्नी की याद स्वाभाविक रूप से आ जाती है
और
उसका अभाव, विछोह मन के पोर-पोर को एक अव्यक्त दर्द
से लबरेज कर देता है। अपनी प्रिया को स्वाभाविक रूप से
याद करते हुए उमाकांत मालवीय कहते हैं
- "टूटे
आस्तीन के बटन / या कुर्ते की खुले सियन
/ कदम-कदम
पर मौके / याद तुम्हें करने के
/ फूल नहीं बदले गुलदस्ते
के / धूल मेजपोश पर जमी हुर्इ/
जहाँ-तहाँ पड़ी दस किताबों
पर / घनी उदासियाँ थमी हुर्इ/
पोर-पोर टूटता बदन /
कुछ
कहने-सुनने का मन / कदम-कदम पर मौके याद तुम्हें करने
के / अरसे से बदला रूमाल नहीं
/ चाभी क्या रख दी जाने कहाँ/
दर्पण पर सिंदूरी छींट नहीं
/ चीज नहीं मिलती रख दी
जहाँ / चौके से आती घुँघुटन
/ सुग्गे की सुमिरनी रटन
/ कदम-कदम पर मौके याद तुम्हें करने के
/ किसे पड़ी
मछली-सी
तड़प जाय / गाल शेव करने में छिल गया
/ तुमने जो कलम एक
रोपी थी / उसमें पहला गुलाब खिल गया
/ पत्र की प्रतीक्षा
के क्षण / शहद की, शराब की चुभन
/ कदम-कदम पर मौके याद
तुम्हें करने के।" उमाकांत मालवीय के इस गीत में
बरसाती नदी का असंयमित उफान नहीं, वरन शारदीया झील के
शांत और निथरे जल की स्निग्ध्ता है। दाम्पत्य प्रेम की
अनेक मनोहारी छवियाँ हैं। जाहिर है कि यह गीत शलभ
श्रीराम सिंह के गीत से भी अधिक विकसित और वस्तुवादी
गीत-संवेदना की उपज है।
आठवें दशक के 'धर्मयुग में शांति सुमन का एक गीत छपा
था- "हाथों में एक-दो मूँगफलियाँ
/ रंगारंग अंतरंग
बातें / यादों में तह करके रख लें हम
/ पार्कों में हुर्इ
मुलाकातें / एक हँसी फेंक कर इधर-उधर
/ दूबों को सहलाना
प्यार
से / पल्लू को स्वत: खिसकने दिया
/ माथ झुका गंधिल आभार से
/ कसी हुर्इ पसीजती हथेलियाँ
/ उमड़-घुमड़ गुजरी बरसातें
/ पिछले पन्ने बरबस खुल गए/
जिन में बीतता समय थम गया/
अनुबंधों को अनुमोदन देने/
होंठों पर एक दस्तखत
नया/ उजले मन की कपास-से रेशे
/ सपनों के और सूत कातें।
शलभ श्रीराम सिंह की मध्यवर्गीय गृहस्थ-वधू यहाँ
आकर आधुनिकता के रंग से सराबोर आधुनिका में तब्दील हो
गयी है। अपना पहला गीत-संग्रह 'ओ प्रतीक्षित को अपने
'पति को, साथ जिये गीतिल क्षणों के लिए समर्पित करने
वाली शांति सुमन इस गीत में उन्मुक्त प्रेम की भोक्ता
और
पक्षधर हो गयी हैं। पार्कों में होने वाली मुलाकातों
में अपने प्रेमी के आगे अपने पल्लू को स्वत: खिसकने
देना,
गंधिल आभार से अपना सिर झुका लेना, प्यार के पिछले
अनुबंधों को होंठों के दस्तखत से सुदृढ़ करना तथा
निश्छल उजले मन की कपास से सपनों के सूत कातने की क्रिया
में उनके उन्मुक्त प्रेम की पक्षधरता स्पष्ट दिखार्इ
देती है।
यह पुरुष सत्तात्मक समाज द्वारा स्त्रियों के उन्मुक्त
प्रेम के अधिकार पर लगाये गए अमानवीय प्रतिबंधें के
विरुद्ध उठा
हुआ प्रतिरोध का तीखा स्वर है। यह उद्दाम
प्रेमाभिव्यक्ति कुण्ठारहित और उदात्त एवं मादक
प्रेमाभिव्यक्ति है, जिसकी
मादकता में माँसलता है लेकिन अश्लीलता नहीं है। इसलिए
शांति सुमन की इस प्रेमाभिव्यक्ति में उत्तर आधुनिक
स्त्री-विमर्श की पदचाप भी स्पष्ट सुनार्इ देती है।
गीत की संवेदना का यह अगला विकास है जो निराला,
महादेवी वर्मा
और शलभ श्रीराम सिंह की संवेदना से भिन्न और केदारनाथ
अग्रवाल की संवेदना का आधुनिक विकास है।
जैसे-जैसे देश और समाज प्रगति कर रहा है, वैसे-वैसे
हमारे सामाजिक और पारिवारिक संबंध और प्रेम की
परिभाषा एवं तरीके भी बदल रहे हैं। आज स्त्रियों की
दुनिया केवल घर-परिवार तक सिमटी नहीं है। आज वे पुरुष
वर्ग के साथ जीवन-संघर्ष में बराबर की हिस्सेदार और
उद्यमी बन गयी हैं। घर में पति और बच्चों की देखभाल करने
के साथ-साथ बाहर कम्प्यूटर और इंटरनेट पर काम करती,
प्रशासनिक पद सम्हालती, न्याय और कानून व्यवस्था
सँभालती, अध्यापन करती, व्यापार करती, संविधान बनाती,
दफ्तर की फाइलें सम्हालती कामकाजी महिलाएँ बन गयी
हैं। इस प्रक्रिया में उनके पास अपने पति या प्रेमी से
जी-भर के प्रेम करने के लिए पर्याप्त अवसर का अभाव
रहता है। इन्हें सिर्फ छुट्टी के दिन ही घर-परिवार के साथ
जीने और प्यार करने का वक्त मिलता है। जिस दिन छुट्टी
होती
है, उस दिन को वह पूरे मन से उत्सव की तरह जीना चाहती
है। ऐसे समय में उनके प्रेम के इजहार का तरीका भी
बदल जाता है। प्रेम की इस बदली हुर्इ संवेदना को
यशोधरा राठौर ने अपने एक गीत में पूरी र्इमानदारी से
चित्रित किया
है- "खुली देर से आँख आज तो छुट्टी का दिन है
/ रही देर
तक सोयी आज न जाना दफ्तर है /
कर्इ दिनों के बाद
मिला मनचाहा अवसर है / अंग-अंग को भिगो रहा खुशबू का
सावन है / जी भर स्नान करूँगी अपने स्वप्न सहेजूँगी
/ बहुत दिनों के बाद गीत छपने को भेजूँगी
/ खोजूँगी रख
दिया कहाँ आया आमंत्रण है / नहीं करूँगी याद आज मैं
दफ्तर
की बातें / नहीं करूँगी याद कि किसने की कितनी घातें
/ घर
के भीतर महक रहा खुशियों का चंदन है
/ कर्इ दिनों के
बाद पेट भर खाना खाऊँगी /
पति से चुहल करूँगी बच्चों से
बतियाऊँगी / रंगों की थापों
पर नाच रहा मेरा मन है।"
यशोधरा राठौर के इस गीत में प्रेम की संवेदना उस तरह
मुखर नहीं है जिस तरह निराला, केदारनाथ अग्रवाल, शलभ
श्रीराम सिंह या शांति सुमन के गीतों में है। इस गीत
में प्रेम का माधुर्य अप्रत्यक्ष, किंतु जीवन-संघर्ष
की मद्धिम उष्मा
से लबरेज है और यह किसी किशोर वय की या युवा स्त्री
का प्रेमाख्यान नहीं है, वरन एक कामकाजी प्रौढ़ महिला
के जीवन-संघर्ष का प्रेमाख्यान है। यह आज की कामकाजी
स्त्री के अनुभवसिद्ध, बड़वानल और जठरानल की भाँति,
अंतर्वर्ती प्रेम की अदृश्य संवेदना है जो समकालीन
प्रेमगीत की संवेदना के विकास का अगला पड़ाव है।
सोवियत रूस के विघटन के बाद निरंकुश अमरीकी
साम्राज्यवाद के अराजक विस्तार, भूमंडलीकृत विश्व-बाजार
और उपभोक्तावादी अपसंस्कृति के अंधाधुंध प्रसार
ने मानव-समाज के सारे सामाजिक, मानवीय और पारिवारिक
संबंधों और रिश्ते-नातों की जड़ें हिला दी हैं। आज
पिता-पुत्रा, माँ-बेटे, भार्इ-बहन और पति-पत्नी के
अंतरंग प्रेम के
बीच में चीजें आ गयी हैं। इसलिए छठे दशक वाली प्रिया
की मर्मस्पर्शी टेर, टेर रही प्रिया, तुम कहाँ-शंभूनाथ
सिंह,
आज उपभोक्ता वस्तुओं की फरमाइश की शक्ल अख्तियार कर
चुकी है। इस उपभोक्तावादी संवेदना का एक गीत देखिए-
"करके टेढ़ी नजर आज तुमने फरमाया है
/ कपड़े धोने
वाली नयी मशीन मँगा दो जी / और एक टेलीविजन रंगीन
मँगा दो जी / डिब्बाबंद मसाले खाने का युग आया है
/ हुए
रसोर्इ-घर के बर्तन सभी पुराने हैं
/ इसीलिए अब नये कुक-वेयर मँगवाने हैं
/ नयी पड़ोसिन ने भी कल ही फोन लगाया
है / वी. सी. आर., फ्रिज फिल्टर, जे. एम. जी. ला देना
/ म्युजिक सिस्टम औ रोटी मेकर मँगवा देना
/ ड्राइंग रूम
बिना सोफा, कूलर भकुआया है /
इस सरदी में मुश्किल गीजर
बिना नहाना है / गाड़ी बिना कठिन बच्चों का पढ़ने जाना
है / नयी सभ्यता ने यह नूतन पाठ पढ़ाया है
/ है सत्तू में
नून
सरीखी ठोहर आमदनी / कर देती बेटी जवान इच्छाओं की छँटनी
/ महँगी की जद से वेतन का
कद कठुआया है।" -नचिकेता।
इस गीत में अंतर्मन का पोर-पोर हिला देने
वाली प्रिया की टेर की टीस या कसक नहीं है, किंतु
ब्याहता
पत्नी की उलाहना-भरी फरमाइशों में जीवन-संघर्ष की दहक
और मिठास अवश्य है। इस गीत में व्यक्त सामाजिक चेतना
में आज की उपभोक्तावादी संस्कृति के बेतहाशा प्रसार के
दबाव की तेज तपिश से मनुष्यों की रागात्मक अनुभूतियाँ
झुलस
गयी-सी महसूस होती हैं। यह आज के समय की अद्यतन और
विकासशील संवेदना है। इस गीत में मध्यम वर्गीय परिवार
की त्रासदी और उपभोक्तावादी आकांक्षाओं के द्वंद्व को
सांकेतिक ढँग से बारीकी के साथ उभारा गया है। ऐसी बात
नहीं
है कि इस दौरान, वर्ष १९५० के बादद्ध महज प्रेम-विषयक
गीतों की संवेदना का विकास और विस्तार हुआ है, बल्कि
गीत की पूरी यथार्थ-दृष्टि, रचना-दृष्टि और जीवन-दृष्टि
में भी कर्इ सकारात्मक और गुणात्मक तब्दीलियाँ आयी
हैं,
जिनकी शिद्दत के साथ गंभीर जाँच-पड़ताल अवश्य होनी
चाहिए। |