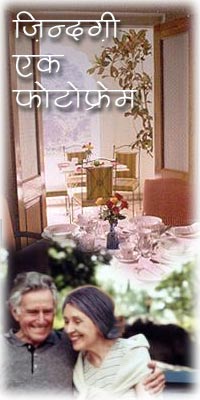 रात का खाना
खाने के बाद अक्सर शैलेश मुझे बालकनी में बुला लेते और ऊपर
आसमान को दिखा कर कहते, "देखो डीयर। आसमान कितना साफ है, तारे
चमक रहे हें मानो उन्हें धो पोंछ कर साफ कर दिया गया हो। वो
सामने देखो चाँद, पूरा नहीं हैं पर दमक कितनी।"
चाँद दिखाते हुए वे आधा बाल्कनी के नीचे लटक जाते। मुझे लगता
कहीं बैलेन्स ना बिगड़ जाये। मैं उन्हें थामने की कोशिश करती ही
रह जाती। वे वापिस मेरी ओर मुड़ते और मुझे अपनी बाहों में थाम
लेते। उनका अन्दाजे.–बयां बच्चों की सी उत्सुकता और उत्साह से
भरा होता। हर दिन वही देख सुन कर भी मैं उस स्पर्श से बच न
पाती। चाहती तो भी पर, फिर मैं चाहती ही कब थी।
असल में, हम लोग तमाम ज़िन्दगी शहर के फ्लैटनुमा घरों में बिता
कर आये थे। वो तो रिटायर होने के बाद ही यह निश्चय किया था कि
गाँव की हवेली में चले जायें। अपना अन्तिम समय तो खुले आसमान
तले, ताज़ा हवा में साँस लेते हुए बिता दें। गाँव की पुरानी
गिरती व झरती दीवारों वाली हवेली में बहुत कुछ ऐसा था जो टूट
कर खण्डहर बन गया था, पर बहुत कुछ ऐसा भी था जिसे सुधार कर
रहने लायक बनाया जा सकता था अतः बना लिया गया था। वहाँ
रहने में एक अजब सी संतुष्टि मिलती थी जिसे शब्दों में बाँध कर
बताया नहीं जा सकता।
शैलेश तो
बेहद प्रसन्न थे इतने कि पिछले बीते चालीस साल भूल ही गये
थे। चाँद तारों में खोये वह एक अजब सुकून का मुजस्सिमा बन
जाते थे। वहाँ रहने में एक अजब सी संतुष्टि मिलती थी जिसे
शब्दों में बांध कर बताया नहीं जा सकता। मैं कभी उन्हें
देखती कभी उनकी उँगली से संकेतित तारों की ओर। वे देर देर
तक चाँद तारों के दिखाते रहते। मेरी गरदन थक जाती पर उनका
देखना बन्द न होता। मैं सोचती रहती इन तारों में क्या
दिखता है उन्हें, पर कभी ना मैंने पूछा, ना ही उन्होंने
बताया।
मुझे अपना बचपन याद आता। वक्त और मौत के हाथों टूट चुके
रिश्ते याद आते। याद आती उनके बीच बसी सोंधी गंध जो घटनाओं
की ढेर–सी परतों के नीचे दबकर धुँधला गयी होती... मैं उन
बीते क्षणों में घुस पड़ती। उन गहराइयों में बड़ा सुकून
बिखरा मिलता। लगता कुछ भी बदले पर इस आसमान का नक्शा तो
वही रहेगा न। अम्मां, बाबा, भैया, भाभी, दीदी, सखियाँ सब न
मिल पातें हों पर हम सबने रात में बैठ कर आसमान की जो
सतरें बचपन में देखी थीं वे आज भी वही हैं। वही ध्रुव
तारा, वही सप्तर्षि, वही पुन्छल तारा...कुछ भी तो नहीं
बदला यह भी खुशी थी। पर यह भी कि यहाँ का आसमान वहाँ के
लोग भी मेरे साथ साथ देख रहे होंगे। सब कोई मेरे करीब आ
जाते और मन खुशी से लबालब हो उठता।
पर उस दिन शैलेश ने मुझे बुलाया। बाल्कनी में रखी बैंच की
पुरानी रंगत वाली उन कुर्सियों पर बैठे शैलेश भी किसी बीते
वक्त से पुराने लग रहे थे। आज वे चंद्र तारों भरे आसमान की
ओर न देख कर कमरे के भीतर झांक रहे थे।
बाल्कनी से घर के कमरे का भीतरी भाग दीख रहा था। यही घर का
सबसे बड़ा कमरा था अंग्रेजी के एल अक्षर की बनावट का।
बाल्कनी की तरफ एल का पतला वाला भाग था, जिसमें शीशम की
लकड़ी की बनी वह डाइनिंग टेबल रखी थी जिस के चारों पैरों पर
ढेर–सी नक्काशी थी। एक–एक पाया हाथी की सूँड की भाँति
दुमुँहा हो रहा था। ऊपर के पल्ले की मोटाई भी छः इंच की तो
रही होगी।
चारों ओर की मोल्डिंग नक्काशीदार जाली से बनी थी। मैं
जानती थी इस तरह के फर्नीचर की सफाई एक बेहद जान लेवा काम
था पर दादा के ज़माने का ये फर्नीचर हमारे लिए शान बघारने
का और आने जाने वालों के लिए ईर्ष्या का वायस भी था।
उस दिन शैलेश ने मेरा हाथ पकड़कर अपने पास बिठा लिया। अपनी
उंगली का संकेत और निगाह की डोर कमरे के भीतर की ओर ले
जाते हुए उन्होंने कहा,
"ज़रा कमरे के भीतर का दृश्य देखो तो।" खिड़की से दिखती वह
डाइनिंग टेबल, सामने रखी मेज़ के कोने में के ऊँचे स्टूल पर
रखा वह फूलदान तथा उसमें सजे कमल के फूल जो यों तो
अर्धमुरझाये थे पर खिड़की के शीशों में से दिखते बड़े
लुभावने और कलात्मक लग रहे थे।
दूर दीखता वह दीवान... दीवान पर बिछी मैरून – केसरिया –
पीले तथा क्रीम कलर के डिजाइन वाली चादर दीवान के ठीक ऊपर
लगी लम्बी–सी पेंटिंग जिसमें नीले पानी की झील के दोनों ओर
हरे भरे पेड़ और पीछे दीखता पहाड़ जिसकी चोटियाँ बर्फ से लदी
थीं... इतना कुछ ही दीख रहा था। मुझे यह दृश्य दिखाते हुए
बोले –
"देखो, कितने खूबसूरत पेंटिंग सा लग रहा है भीतर के कमरे
का ये दृश्य। ये गमला आगे की ओर... दूर पर लगी वह पेंटिंग
का दृश्य... त्रिआयामी... अपना ही घर किसी तस्वीर सा
खूबसूरत...सोचा भी नही कभी।"
मैं चुपचाप देखती रही। शैलेश फिर बोले, "और ये जो गमला दीख
रहा है न...इससे ये पेन्टिंग खासा पुराने वक्त की बनी दीख
रही है।"
अपना बैठने का कोण बदलते हुए वे फिर बोले, "क्या कहोगी।
सत्रहवीं शती के किसी पेन्टर की।"
शैलेश सही थे। कई कारणों से वह पेन्टिंग ही लग रही थी।
खिड़की के चारों ओर की चौखट फ्रेम बन गयी थी। भीतर धुँधली
परछाइयाँ बनाती रोशनी, गमले का सरसों सा पीलाया रंग, जो
पुराना पड़ मटमैला हो कर उसे सत्रहवीं शती का बना रहा था
फिर कमल के फूल जो अपना रंग वा ताज़गी खो चुके थे। मेज़ पर
मिट्टी का जग भी तो रखा था। छत के बीचों बीच लटका पुराना
दादा जी के ज़माने का झूमर... अपनी ढेर सी काँच की झालरों
के साथ धमक मार रहा था। झूमर दादाजी के ज़माने का था,
मिट्टी का जग पिछली बार जयपुर से आये मित्र ने भेंट किया
था जिस पर मीनाकारी की हुई थी। तिस पर वह मटमैले पीले रंग
का गमला।
गमला देखकर मन में कसक उठी। उस गमले से अब कोई सम्बन्ध बचा
तो नहीं था फिर भी वह कहीं न कहीं मन में तिरछा जा चुभता
था। ये भी सच है कि दिनभर में अनेक बार उसे देखकर कुछ नहीं
उगता था। उस दिन जब शैलेश ने भीतर के दृश्य की पेन्टिंग
बना कर रख दी तो गमला भी पेन्टिंग बन कर जे.हन में उतर
गया। गमले वाले की याद आना तो लाज़िमी था। सामने का दृश्य
सचमुच लुभावना था...इतना लुभावना कि लगा अगर किसी पत्रिका
में ऐसी फोटो देखती तो सचमुच में काट कर रख लेती, अपनी
फाइल में या फ्रेम करा कर किसी को गिफ्ट करने के लिए तैयार
कर लेती। ऐसा करना मेरी आदत में शुमार था। और कुछ न होता
तो कम से कम अपनी मेज़ पर के शीशे के नीचे तो अवश्य रख
लेती। इतनी खूबसूरत पेन्टिंग दुनिया में फैली खूबसूरती का
अहसास दिलाती रहती। पर फिर यह भी सोचती रहती कि कैसे होते
होंगे वे घर जिनमें ऐसी पेन्टिंग्स होती होंगी। क्या क्या
होता होगा उन लोगों के घर में? उन सब की कल्पना करती जो जो
चीज़े उनके घर में होती होंगी। कमल के फूल अपनी नाल के
झुकने से झुके हुए थे। उन्हें देखकर मेरी कल्पना ने पींगे
बढ़ाई। मुझे लगा मानों नाल और फूलों के बीच होड़ लगी हो। नाल
फूल को नीचे लाना चाहती, फूल ऊपर जाने का इसरार करते तने
खड़े रह रहे थे। मैंने चाहा तो अनेक बार कि गमले में नकली
फूल लगा दूँ – हर वक्त की झिकझिक खत्म, पर कभी मन मान ही
नहीं पाया। हमेशा नये फूल लाये जाते उनमें नमक ताँबे का
सिक्का डाला जाता फिर
भी वे चार पाँच दिन बाद बदलने पड़ते ही।
उस तस्वीरनुमा कमरे में झांकती मेरी निगाह गमले पर टिकी
रही थी। पार्थ याद आये। गमला और पार्थ मिल कर एक हो गये।
पार्थ कपूर..."ये नाम शरीर व मन के भीतर कहीं धंसा पड़ा
था... गहरे चीरता हुआ।... "क्या करूँ उसका" मैं सोचती रहती
। जिनको हम भुलाने की कोशिश हमेशा करते हैं उन्हें ही तो
नहीं भुला पाते।
"पार्थ आज तो मेरी ज़िन्दगी में नहीं हैं फिर मैं क्यों
उनसे जुड़ी हूँ। पर क्या सचमुच नहीं जुड़े? फिर क्यों ये
गमला तान्या को नहीं दे पाती। तान्या शैलेश की पुत्री
है... क्या इसलिए? क्यों मैं चाहती हूँ कि ये गमला पार्थ
के पुत्र सुसीम के ही पास जाये।"
किसी बात का कोई जवाब नहीं था। होता भी क्या। जवाब वह
चाहती भी कहाँ थी।
जहाँ ये सच है कि सब बातों के उत्तर हो नहीं सकते वहाँ ये
भी सच है कि हमें मालूम होते हैं...मन में छिपे वे जवाब
जो उस स्थिति में
निश्चित थे।...पर फिर क्या सब कुछ जान लेना इंसान के बस
में होता है।
टेलिफोन की आवाज़ थी। मैं तस्वीर से बाहर निकल आई। घंटी ज़ोर
ज़ोर से बज रही थी। अभी तक तस्वीर में टेलिफोन का चोंगा
नहीं दिखा था। ऐसा लगा जैसे वह ज़ोर ज़ोर से बज कर अपने होने
का अहसास दिला रहा था।
"पर मैं...मेरे होने का अहसास...मैं क्यों नहीं दिला पाती
अपने होने का अहसास। सभी मुझे 'टेकन फॉर ग्रान्टेड' लेते
हैं। और मैं...उनकी माँग पर सही उतरने की कोशिश में खुद को
फ्रेम में लगी तस्वीर बनाती जा रही हूँ।...अपने लिए अपने
तरीके से कुछ भी सोचने की मुमानियत भरी दीवार अपने चारों
ओर बनाती...अपने अहसासों से बहुत दूर...अवांछाओं के बीच।"
मैं उठ तो गयी थी। टेलिफोन की तरफ चल भी दी थी पर मन के
भीतर जो कुछ चल रहा था उससे कैसे बच पाती।
"हमेशा मन भरी गगरी सा भरा रहता है, छलक पड़ने को
तैयार...जब बोलने का मौका मिलता तेज़ी से घूमती गगरी की
भाँति एक बूँद भी न छलकती।"
ऐसा क्यों हैं कि समस्त वैज्ञानिक नियम तक जिन्दगी पर सही
उतरते हैं। लाख चाहती कि मन की गागर थोड़ी खाली कर दूं शायद
तब भावों को छलकने में आसानी होगी। पर जो चाहती वह...कभी न
कह पाती। और जो कह पाती वह
सामने बैठे इन्सान से इतना
प्रभावित होता कि उसी के अनुकूल दिमाग सोचने लगता...न
चाहते हुए भी।
फोन शैलेश की पुत्री तान्या का था। पार्थ से अलगाव के
पश्चात् सुसीम को संभालती जब मैं अकेली इस संसार सागर में
तूफानी लहरों से जूझ रही थी तभी मेरा सामना शैलेश से हो
गया था जो अपनी पत्नी के मृत्यु के पश्चात् अपने दोनों
बच्चों को संभालने का कठिन कार्य कर रहा था बल्कि जूझ रहा
था कहना अधिक सही होगा।
अपने अपने गमों और तकलीफों तथा अपने बच्चों से मिलने वाले
ढेर से दुखों और खुशियों में डूबते उतराते हम बच्चों के
कैम्प में टकरा गये। यों भी कहा जा सकता है कि नियति ने
मिला दिया।
अब तो इस बात को चौबीस साल हो गये हैं। सफर के सब दुखद पल
भूल गये हैं। हाँ, कुछ कुछ याद है...नमकीन चटपटे लम्हें।
मेरा और शैलेश का बेटा शुभीश और बेटी शुभाशा बड़े होकर
यूनिवर्सिटी चले गये हैं। हम रिटायर हो गये हैं तथा अपने
गाँव के बड़े से घर में अपना छोटा सा बच्चों विहीन वजूद
समेट रहे हैं।
टेलिफोन पर बात करती हुई मैं लगातार उस गमले के झरते और
मटमैले पड़ते रंगों में खो गयी थी। अजीब सा सच है कि पैंतीस
वर्ष बीत गये पर पार्थ की याद की खाई न भरी, न मटमैली
धुँधली पड़ी। रिश्तों की नींवें इतनी मज़बूत होती हैं। पर
प्रायः यह सच भी नहीं होता।
टेलिफोन पर तान्या से
सामान्य बातचीत हुई जो हालचाल पूछने तथा स्वास्थ्य एवं
पढ़ाई की चिन्ता से जुड़ी थी। शैलेश दरवाज़े पर खड़े थे।
उन्हें देखकर ही मैंने कहा था,
"सुनो तान्या, तुम्हारे पापा यहीं खड़े हैं, उनसे बात करो।
ओ.के. बाय। टेक केयर।" कहते हुए मैंने फोन शैलेश को दे
दिया। फोन थामते हुए शैलेश ने अपनी वही पुरानी हरकत
दोहराई। वे हमेशा कहते कि फोन का चोंगा पकड़ाते हुए उन्हें
हमेशा हमारी शादी के एकदम बाद वाला चेहरा याद आता। जाने
क्या था चेहरे के उस कोण में जो उन्हें आकर्षित करता।
मुझे लगा ये भी जिन्दगी के किसी एक क्षण, चेहरे के एक कोण
को, उस पर दिखने वाले किसी एक भाव को फ्रेम करने जैसा ही
तो था। फोन का चोंगा लेते हुए शैलेश ने पीछे हटती मुझे
हल्का सा छुआ और एक चुम्बन मेरे भाल के पास से गुजर गया।
मैं झेंप गयी थी। मुझे याद है पहले मैं पानी में भागती
मछली सी उनकी पकड़ से छूटती और फिसल जाती पर अब, अब अक्सर
उन्हें हल्का सा धकियाती उनके उस चौड़े सीने पर हाथ रखती
थामती फिर निकल जाती। उस दिन जब शैलेश ने चोंगा पकड़ते हुए
मुझे अपनी बाहों के दायरे में लिया तो मैंने उन्हें पीछे न
धकेला। उनके सीने से लता सी लिपटी रही। पार्थ को भी वहीं
कहीं आस पास महसूसते हुए।
आंधी भरा मन थमा तो धीमे से अपने को अलग करती हुई फिर से
बाल्कनी की अँधियारी सुरंग में डूबने लगी। सामने की तस्वीर
फिर आंखों के कोरों में सिमट आई। जिन्दगी को किसी दौर में
सीखी पेन्टिंग कला जोर मारने लगी। सोचने लगी कि अगर मैं
सामने वाले दृश्य को कैन्वास पर उतारूँ तो कितना मज़ा
आयेगा। सोच कर खुशी के इन्तहा दरवाज़े
खुल आये। पर...क्या मैं इतनी
ही गहराई दे पाऊँगी।
विभिन्न कोणों से खिड़की के भीतर झाँकती हुई मैं सोचती रही।
अचानक मन में निराशा जन्मी। आखिर कैन्वास पर ढली पेन्टिंग
में नज़रिया किस का भरेगा? क्या मेरा या फिर उसका जो इसे
देखेगा। व्यक्तिगत नज़रिए कितने महत्वपूर्ण होते हैं इसे
क्या नकारा जा सकता है।
तभी...तभी तो पार्थ से अलग होते हुए रिश्तेदार दोस्त यही
समझते रहे थे कि ये सब एक मज़ाक है जो वक्त के साथ दम तोड़
देगा। पर...कहाँ। पार्थ मुझमें वह सब न देख पाये जो वह
देखना चाहते थे। सुसीम का जन्म हो चुका था फिर भी। अपने
व्यक्तित्व को, अपने नज़रिये को महत्व देने का गुण पार्थ ने
विदेश से सीखा था।
अजब होता है इन विदेशियों का नज़रिया भी। उनके लिए 'मैं
इतना प्रिय होता है कि उसके सम्मुख 'पर' की कोई जगह ही
नहीं बच रहती। फिर उनमें ये गुण भी तो नहीं है कि 'पर' का
'स्व' बना पाये। पर फिर...ये लोग इतनी समाज सेवा कैसे कर
पाते हैं। ये बात मुझे हमेशा आश्चर्यचकित करती रहती।...जब
जब मैं विदेश में रहने जाती... एक और प्रश्न मेरे भीतर
कुलबुलाता रहता। अपने बच्चों के लिए अपनी नौकरियों तक को
छोड़ कर बच्चों को बड़ा करने वाले यही माता पिता आपस में ज़रा
सा तनाव होने पर उन्हें पेड़ से टूटती–सूखती टहनी–सा छोड़कर
अलग थलग जा खड़े ही नही होते अपितु किसी दूसरे का साथ ढूंढ
कर उसका हाथ थाम लेते हैं और चल देते हैं... दूसरी राह पर।
कैसे और क्यों। कौन सा
मनोविज्ञान इसकी व्याख्या
करेगा।
कभी–कभी मुझे लगता कि ये लोग वास्तविक अर्थ मे वैरागी हैं
जो जब तक जिस परिस्थिति और वातावरण में होते हैं पूरी तरह
उसी में ज़ज्ब होते हैं और उससे बाहर निकलते ही छिटक कर जा
पड़ते हैं...दूर...बहुत दूर... इतना दूर...समस्त स्थिति से
प्रभावहीन।
बरसों–बरस विदेश में बसे पार्थ भी इस अलगाव भाव से जुड़ गये
थे तभी तो शायद...तभी तो इधर हम अलग हुए उधर निशा नामक
लड़की जो उनके ही आफिस में काम करती थी विशुद्ध विदेशी
तहज़ीब में रंगी पगी से विवाह रचाया और घर बसा कर उसी में
रम गये।
शैलेश को चेहरे पर की मुस्कान से ही पता चल गया था कि अब
आखिरी 'बाई' 'विश यू गुड लक' आदि वाक्यों का आदान प्रदान
हो रहा था।
फेन रखकर शैलेश यहीं आने वाले थे...बाहर बाल्कनी में ।
ख्यालों की बहती बयार से मैं बाहर निकली। वर्तमान में लौट
आई। पार्थ से जुड़ी। खुद को उससे काटने की कोशिश मे कुछ
असहज भी। शरीर में बेचैनी भर उठी थी। ऐसे में शैलेश का पास
होना सुकून देता था।
शैलेश आये तो मानों आंधी थम गयी। उन्होंने आते ही बातों की
डोर का सिरा फिर से थाम लिया।
'हाँ तो मैं क्या कह रहा था। येस। हमारी पेन्टर की निगाह
कैसी लगी। चित्रकार को अब मंच पर आकर अपनी बात
कहनी चाहिए।'
मैं हंस पड़ी। अचानक लग उठा कि मेरा मन तो इतने सारे
ख्यालों के भार को नीचे दबा पड़ा है कि अपनी बात कहने के
लिए शब्द कहाँ खोजूँ ? और बोलूँ क्या?
'कोई जाने तो मैं क्या कहना चाहती हूँ। पर...कोई जाने
क्यों। अगर कोई जानना चाहे तो क्या मैं बता पाऊँगी। मेरे
पास शब्द ही कहाँ हैं... इतने ढेर सारे शब्द जो मेरे
खयालों को समेट सकें। जो शब्द हैं वे काफी नहीं है।
फिर...शब्द ढूंढ भी लूं तो क्या अपनी बात कह पााउंगी। आज
तक तो कह नहीं पाई। 'सोचती रही थी।' पार्थ सुनने कहने से
पहले चले गये थे। उसके बाद...उसके बाद कहने की आदत ही छूट
गयी।'
शैलेश ने प्रश्न पूछा था। उत्तर की अपेक्षा करते बैठे थे।
उन्हें अपनी ओर देखता पाकर ही में बोली थी,
'हिष्ट। शैलेश। मैं कोई पेन्टर बेन्टर नहीं हूँ। वे तो
बचपन की बातें हैं बचपन के साथ बीत गयीं। जो बीत जाता है
हम उसी के लिए तरसते हैं। अब देखो न! किसी खूबसूरत तस्वीर
को देखते हैं तो उसकी तुलना ज़िन्दगी से करते हैं और
ज़िन्दगी की उपमा खूबसूरत
तस्वीरों से करने लगते हैं। नहीं क्या।'
शैलेश की निगाह में
क्या था बताना कठिन था। उन्होंने मुझे अपने सीने से लगाते
हुए मेरा चेहरा खिड़की की ओर कर दिया। उस ओर देखते हुए
बोले,
'ठीक कहती हो। अब देखो न! कमरे के भीतर से देखें तो शायद
हम यहाँ इस पोज़ में फ्रेम के भीतर लगे 'पोर्ट्रट' से दिखाई
देगे। सच तो ये है कि हम सभी ज़िन्दगी और फ्रेम की तस्वीर
दोनों ही साथ साथ जीते हैं। वक्त आगे भागता है और तस्वीरें
पीछे छोड़ जाता है। यही तो जीने का मज़ा है और यही जीने का
सबसे अच्छा तरीका भी है।'
मैं शैलेश के सीने से चिपकी हैरान उनका मुँह देख रही थी।
आखिर मैं क्यो नहीं कह पाती यह सब। शैलेश ने कैसे वह सब
आसानी से कह दिया जिसके लिए मैं शब्द ही खोजती रही थी।
मैं...मैं अभी तक पार्थ के साथ बीते वक्त को फ्रेम में जड़ी
तस्वीर नहीं बना पायी थी। तभी...तभी तो उसके बदरंग दाग जब
तब सीने में टीसते रहते हैं। मैंने सोचा तो यही था पर बोली
थी,
'हाँ! तभी तो बीता समय हमारे भीतर एक त्रिआयामी क्या
चतुर्आयामी तस्वीर बन जाता है। और तभी बदरंग क्षण तस्वीर
की तरह अच्छे लगते हैं या फिर इसलिए कि हम उसे बीती
शताब्दियों की तस्वीर समझ लेते हैं।'
शैलेश के सीने मे समाया मेरा वजूद वहीं ठहर गया था
फोटोफ्रेम बन... पर ज़िन्दगी भी तो यही कहीं टहल रही थी।
ये सफर विदेश से स्वदेश लौटने का नही था... शहर से अपने
गाँव चले आने का नहीं था. ये तो ज़िन्दगी के भीतर जाकर पुनः
ज़िन्दा हो जाने का सफर था...कभी ना खत्म होने वाली अद्भुत
अनुभव यात्रा थी। अनुभवों का ना तो कोई रंग होता है न रूप
न गन्ध। वे तो ज़िन्दगी के साथ जुड़े होते हैं...अकाट्य रूप
से।
|